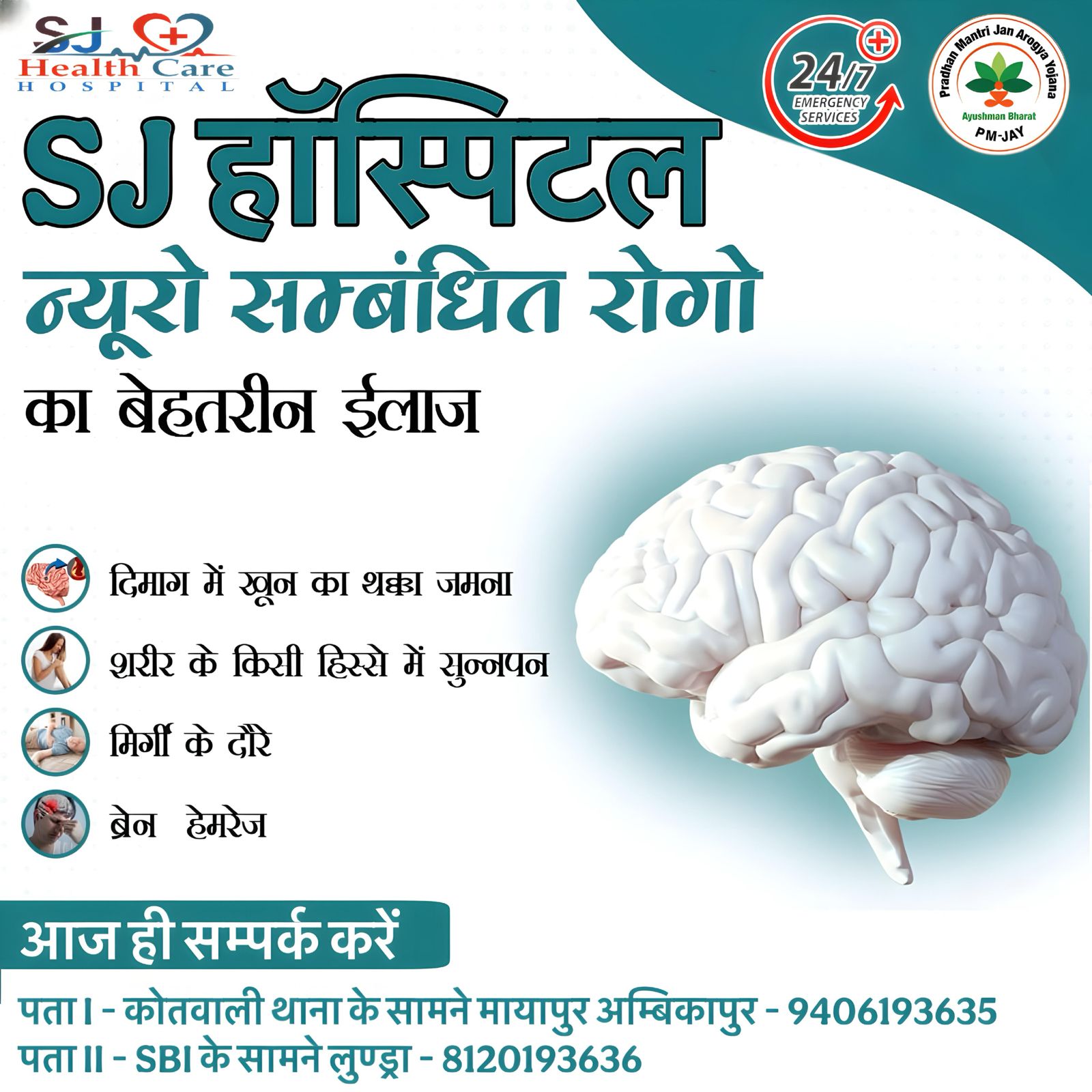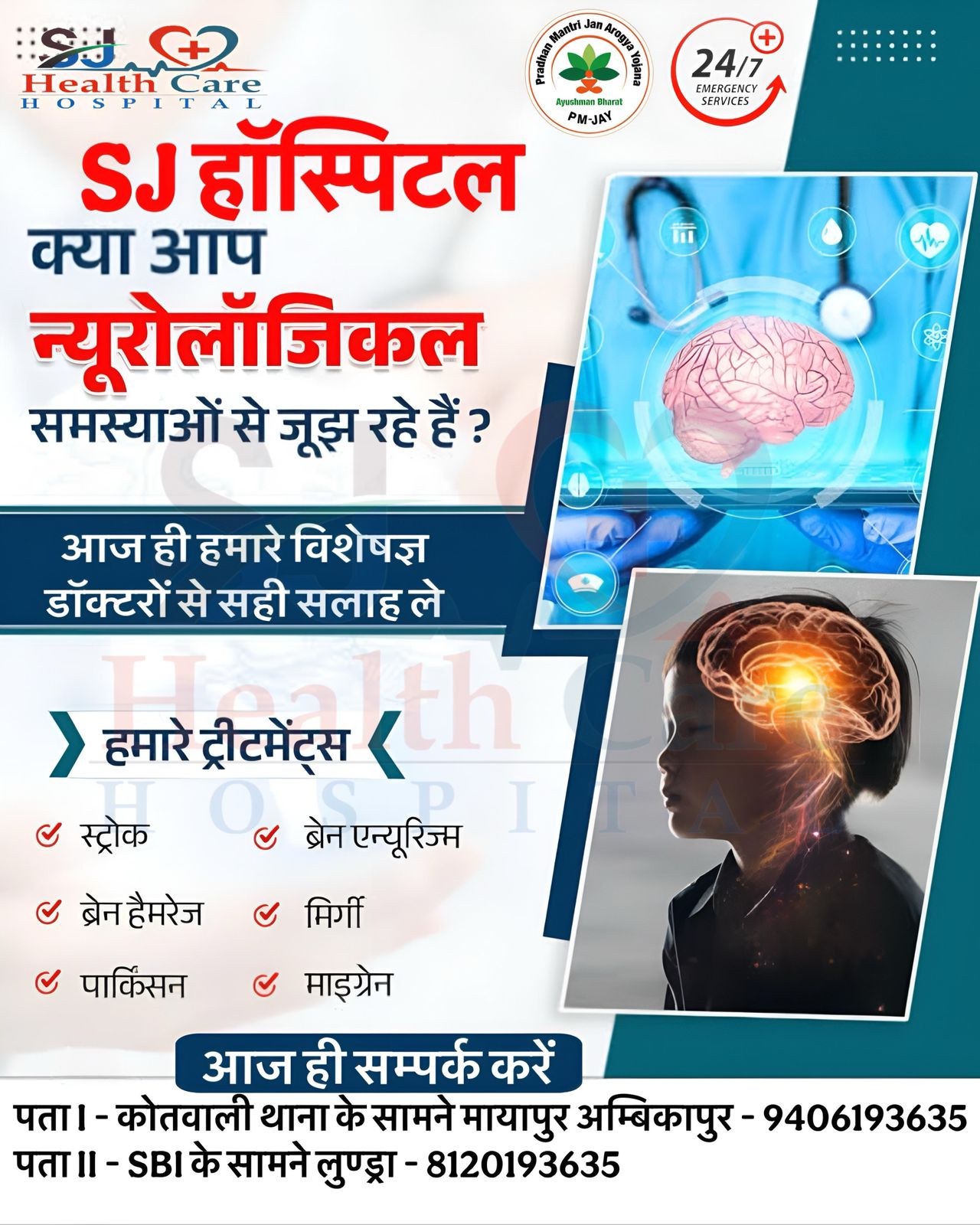उत्तराखंड में एक के बाद एक गाँव क्यों हो रहे हैं ख़ाली
उत्तराखंड में एक के बाद एक गाँव क्यों हो रहे हैं ख़ाली
पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील के किमगिड़ी गाँव की महिलाएं अपने खेतों में मंडुआ, उड़द और अन्य दालों की कटाई कर रही हैं.
17, 18 और 19 अक्टूबर को लगातार भारी बारिश की मार खेतों में खड़ी दाल की फ़सल पर पड़ी है.
बुज़ुर्ग किसान लीला देवी कहती हैं, “जब बारिश चाहिए तब नहीं होती. अभी बेमौसम की बारिश हो रही है. उड़द की दाल गल गई है. मंडुवा सड़ गया. पशुओं के चारे के लिए हमने घास काटकर रखे थे, वो भी सड़ गई.”
वह बताती हैं कि मई में बुवाई के समय भी लगातार बेमौसम बारिश हुई थी. जिसका असर पौधों पर पड़ा और अब कटाई के दौरान बारिश ने रही-सही कसर पूरी कर दी.
लीला देवी अपने खेतों का वो हिस्सा भी दिखाती हैं, जिसमें जंगली सूअरों के झुंड ने नुक़सान पहुँचाया है.

वह कहती हैं, “कुछ मौसम के चलते खेती ख़राब हो जाती है. कुछ जानवर खा जाते हैं. अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है”.
वह दिखाती हैं, “पहले हमारे खेत दूर तक फैले हुए थे. हम वहाँ तक खेती करते थे. लेकिन अब हमने सब छोड़ दिया है. हमारे खेत बंजर हो गए हैं. हमारी बेटियां-बहुएं कहती हैं कि हम कैसी भी नौकरी कर लेंगे लेकिन दराती-कूटी नहीं पकड़नी. हमने तो इसी खेती से अपने बच्चे पाले. गाय-भैंस पाले. सबका भला किया.”

“इससे अच्छा तो नौकरी करना है”
लीला देवी अपने परिवार की आख़िरी किसान रह गई हैं. उनका एक बेटा देहरादून और दूसरा जोशीमठ में नौकरी करता है.
लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के अनुभव के आधार पर वह कहती हैं, “एक दिन जब उन्हें नौकरी में लाभ नहीं होगा तो वे ज़रूर यहाँ वापस आएंगे, कुदाल पकड़ेंगे, हल लगाएंगे.”
पूनम बिष्ट इन्हीं खेतों में उड़द, मूंग, सोयाबीन की कटाई कर रही हैं. उसने चौबट्टाखाल डिग्री कॉलेज से बीएससी की है.
वह कहती हैं, “खेतों में काम करके कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. इससे अच्छा तो नौकरी करना है.”
जलवायु परिवर्तन का असर
उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के दबाव के चलते लोग खेती छोड़ रहे हैं और नौकरी के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं.
द एनर्जी ऐंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट और पॉट्सडैम इंस्टिट्यूट फ़ोर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च की इस वर्ष जारी शोध रिपोर्ट के मुताबिक़ आने वाले वर्षों में इसमें अधिक तेज़ी आएगी.
उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग ने भी राज्य में बंजर हो रहे खेत और पलायन को लेकर जारी अपनी रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी वजह माना है.
वर्ष 2019 में आई पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक़ उत्तराखंड की 66% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. इसमें से 80% से अधिक आबादी पर्वतीय ज़िलों में हैं.
पहाड़ों में किसानों की जोत बेहद छोटी और बिखरी हुई है. यहाँ सिर्फ़ 10% खेतों में सिंचाई की सुविधा है. बाकी खेती मौसम पर निर्भर करती है.
वर्ष 2001 और 2011 के जनसंख्या आँकड़ों के मुताबिक़ राज्य के ज़्यादातर पर्वतीय ज़िलों में जनसंख्या वृद्धि दर बेहद कम रही है. इस दौरान अल्मोड़ा और पौड़ी ज़िले की आबादी में 17,868 व्यक्तियों की सीधी कमी दर्ज की गई है.

मात्र एक परिवार वाला गाँव
चौबट्टाखाल तहसील के ही मझगाँव ग्रामसभा के भरतपुर गाँव में रह रहा आख़िरी परिवार इन रिपोर्टों को सच साबित करता हुआ मिला. गाँव के ज़्यादातर घर खंडहर बन गए हैं. कुछ घरों पर ताले तो कुछ के टूटे किवाड़ और उनके अंदर तक झाड़ियां उगी हुई दिखीं.
गाँव के खेत झाड़ियों में छिप गए थे. यशोदा देवी यहाँ अपने पति, बहू और उसके तीन छोटे बच्चों के साथ रहती हैं. दो बेटे दिल्ली और गुड़गाँव में नौकरी करते हैं. पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो बहू अपने बच्चों के साथ वापस लौटी हैं.
वह बताती हैं, “गाँव में हमारा अकेला परिवार रह गया है. कभी शादी-ब्याह या पूजा के समय दो-चार दिनों के लिए लोग आते भी हैं. कई ने तो हमेशा के लिए ही गाँव छोड़ दिया है.”
यशोदा देवी ने अपने घर के चारों तरफ़ कई बल्ब लगाए हैं ताकि रात के समय रोशनी से गुलदार घर के नज़दीक न आए.
वह कहती हैं, “तीन-तीन बघेरा (गुलदार) हमारे घर के सामने चक्कर लगाते रहते हैं. चार दिन पहले ही उसने हमारे बछड़े को मार दिया. हमें अपने छोटे बच्चों का भी डर लगा रहता है. वन विभाग वालों को बोलो तो वे कहते हैं कि अपने घर के आसपास झाड़ी काटो, सफ़ाई करो. हम कितनी झाड़ियां काटेंगे.”
खेती के बारे में पूछने पर वह बताती हैं, “जो खेती करते हैं वो सूअर ले जाता है. तीन दिन लगातार बारिश लगी थी. बिजली नहीं थी. सूअर का झुंड खेतों में घुस आया. उन्हें भगाने के लिए रात में कौन बाहर जाता. अब तो ऐसा हो गया है कि बरखा लगती है तो बरखा ही लगी रहती है, घाम पड़ता है तो घाम ही होता रहता है.”

ये गाँव भी खाली हो जाएगा!
भरतपुर गाँव से आगे नौलू गाँव भी पलायन की मार झेल रहा है. गाँव के ज़्यादातर परिवार शहरों में बस गए हैं.
यहाँ के किसान सर्वेश्वर प्रसाद ढौंडियाल कहते हैं, “अगले दो-तीन साल में हमारा गाँव भी भुतहा हो जाएगा. कुछ परिवार अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने की वजह से जा रहे हैं. तो कुछ चौपट हो चुकी खेती और जंगली जानवरों के आतंक के चलते.”
वह बताते हैं, “एक समय ऐसा था कि हमारे खेतों में इतना लहसुन, प्याज़ और मिर्च होता था कि बेचना मुश्किल हो जाता था. मेरे खेत भरे रहते थे. हम धान, कोदा, झिंगोरा, गेहूं, दाल, भट्ट, गहत समेत बहुत कुछ उगाते थे. लोग हमारे घर आते थे तो हम उन्हें दाल-मंडुआ देते थे. अब कुछ नहीं होता. गाँव के जल स्रोतों में पानी बहुत कम हो गया है. इससे खेतों में सिंचाई मुश्किल है. जो थोड़ी-बहुत खेती करते हैं, उसे जानवर नहीं छोड़ते.”
सर्वेश्वर अपने घर की छत पर सूख रही उड़द समेत अन्य दालें दिखाते हैं, “जंगली सूअरों ने इनमें कुछ दाने नहीं छोड़े हैं. हमारे परिवार के लिए भी अनाज मुश्किल ही होगा. पहले सब लोग खेती करते थे. तो जानवर से जो नुक़सान होता था वो सबका थोड़ा-थोड़ा होता था. अब कुछ ही खेत रह गए हैं तो चिड़िया भी वहीं आती है, जानवर भी वहीं आते हैं, इंसान को भी उसी से गुज़ारा करना है.”
वह उम्मीद जताते हैं कि अगर सरकार हमारे बच्चों को यहीं पर रोज़गार देती तो पलायन नहीं करना पड़ता. बहुएं घरों में रहतीं तो खेत भी हरे-भरे रहते. “ये हमारी देवभूमि है. हम क्यों अपनी मिट्टी से दूर जाते.”
हरियाणा में पली-बढ़ीं निर्मला सुंद्रियाल 13 साल पहले शादी के बाद पौड़ी के कुईं गाँव रहने आईं. उनके गांव में कभी 80 परिवार हुआ करते थे. अब 30 परिवार रह गए हैं.
चूल्हे पर रोटी पकाती हुई निर्मला कहती हैं, “गाँव में जब ज़्यादा लोग थे, खेत हरे-भरे रहते थे, झाड़ियां नहीं होती थीं, जंगली जानवरों की इतनी समस्या नहीं होती थी. अब कम लोग रह गए हैं तो बचे खुचे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. जिन पहाड़ों पर खेती होती थी वहां चीड़ के जंगल उग आए हैं. गर्मियों में इन जंगलों में आग लगती है तो भी जानवर हमारे गाँवों की ओर आते हैं. जंगल में उन्हें भोजन-पानी नहीं मिलता, इसलिए वे हमारे पशुओं को निवाला बनाते हैं.”

खेती और जलवायु परिवर्तन
जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ तेज़ प्रताप कहते हैं. “अब हम उस दौर में पहुँच गए हैं, जहां खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर बिलकुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है. पहले ये कहा जाता था कि ग्लोबल वॉर्मिंग होगी तो जो फ़सलें जहाँ उगती हैं, उससे अधिक ऊंचाई पर शिफ़्ट हो जाएंगी. मौसम हमें बता रहा है कि तापमान बढ़ने के साथ बारिश और बर्फ़बारी का पैटर्न भी बदल गया है.”
“इस साल मई में गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा बारिश हुई. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी मई में ऐसी बरसात देखने को मिले. मौसम में आ रहे बदलाव बेहद अप्रत्याशित हैं. इससे किसानों को ये नहीं पता चलेगा कि बीज कब बोए जाने हैं. बीज बो दिया और उसके बाद तेज़ बारिश हो गई तो फ़सल ख़राब हो जाएगी. बीज बोने के समय पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो भी फसल को नुक़सान पहुंचेगा.”

ऐसे दिनों की संख्या बढ़ रही है जब तापमान 50 डिग्री या उससे ज़्यादा हो रहा है.
“हम पिछले 10-15 सालों से बुवाई के समय और बारिश के पैटर्न में आ रहे इन बदलाव पर ग़ौर कर रहे हैं. ये समय फ़सल की कटाई का था और अक्टूबर में हुई अप्रत्याशित बारिश से किसानों की उपज प्रभावित हुई है.”
डॉ तेज़पाल कहते हैं, “ये तय है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से आने वाले समय में तीव्र मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी और एक लंबा समय सूखा बीतेगा. हमें कृषि के लिहाज से इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने की तैयारी करनी होगी.”
स्टेट ऑफ़ इनवायरमेंट रिपोर्ट ऑफ़ उत्तराखंड (2019) के मुताबिक भी जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है. तापमान बढ़ने, अनियमित बारिश, मानसून में देरी, सिंचाई के स्रोतों के सूखने जैसी वजहों से राज्य में कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है.

क्या जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा है मानव-वन्यजीव संघर्ष?
वन्यजीवों के लिए कार्य कर रही संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट प्रोग्राम में डायरेक्टर डॉ. दीपांकर घोष कहते हैं, “सीधे तौर पर हम जलवायु परिवर्तन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को जोड़ नहीं सकते. लेकिन ये स्पष्ट है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं.”
”इससे जंगल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. ऐसे पेड़-पौधे जिनके फल-फूल पर जंगली जानवर निर्भर करते हैं, वो यदि जंगल की आग में ख़त्म हो जाएंगे तो वन्यजीवों को भोजन की दिक्क़त आएगी. हालांकि इस पर बहुत कम शोध हुआ है.”
देहरादून में वाइल्ड लाइफ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया में वैज्ञानिक डॉ बिवाश पांडव कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के असर से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं. वह उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भालू के साथ बढ़ते संघर्ष का उदाहरण देते हैं.
वे कहते हैं, “भालू पहले 4-5 महीने शीत निद्रा में रहते थे. लेकिन बर्फ़बारी कम होने से शीत निद्रा का उनका समय घट रहा है. लद्दाख के द्रास और जांस्कर घाटी में हमने पाया कि भालू एक महीना भी शीतनिद्रा में नहीं जा रहा.”

जलवायु परिवर्तन से इंसानों को ख़तरा: यूएन
लेकिन पौड़ी समेत मध्य हिमालयी क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को वे सामाजिक समस्या मानते हैं.
वे कहते हैं, “पलायन होने, खेत बंजर होने, खेतों की देखभाल के लिए पर्याप्त लोग न होने की वजह से पहाड़ों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं. मान लीजिए जंगली सूअर के झुंड पहले 100 एकड़ में खेती को नुक़सान पहुँचाते थे, अब 40 एकड़ में खेती हो रही है तो हमें नुकसान की तीव्रता ज़्यादा लग रही है. खेत बंजर होने से झाड़ियां भी बढ़ गई हैं. जिसमें गुलदार जैसे जानवर आसानी से छिप जाते हैं और गाँव के नज़दीक पहुँच रहे हैं.”
पिछले वर्ष लॉकडाउन में लौटे गुड्डू देवराज (पीली टीशर्ट में) बरसों से बंजर पड़े अपने खेत आबाद करने में जुटे हुए हैं
विपरीत हालात में भी लौटने वाले लोग
गुड्डू देवराज पहाड़ की बंजर हो चुकी ढाल को आबाद करने में जुटे हैं. वर्ष 2020 में कोरोना काल में वे पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के अपने गाँव गडोली वापस लौटे.
वह बताते हैं, “दिल्ली में क़रीब 35 वर्ष बिताने के बाद जब हम अपने गाँव पहुँचे और पुरखों की ज़मीन बंजर देखी तो बहुत दुख हुआ. शहर से गाँव लौटनेवाले क़रीब 15 प्रवासियों ने फ़ैसला किया कि अपने बंजर खेत आबाद करेंगे.”
”पिछले वर्ष जून में हमने काम शुरू किया था. लेकिन इस वर्ष जून तक हम सिर्फ़ 5-6 लोग ही यहाँ रह गए हैं. बाक़ी सभी दोबारा शहर चले गए. इन एक डेढ़ साल में हमने अपने खेतों में क़रीब 200 किलो टमाटर और 200 किलो लहसुन समेत अच्छा उत्पादन किया.”
इन 35 सालों में गाँव में क्या बदला? इस पर वह कहते हैं कि कभी यहाँ हिस्सर, किमगोड़ा, सेमल समेत जंगली फल हुआ करते थे. लेकिन धूप-छांव-बारिश का समय बदला है. शायद इसी से वे लुप्त हो गए.