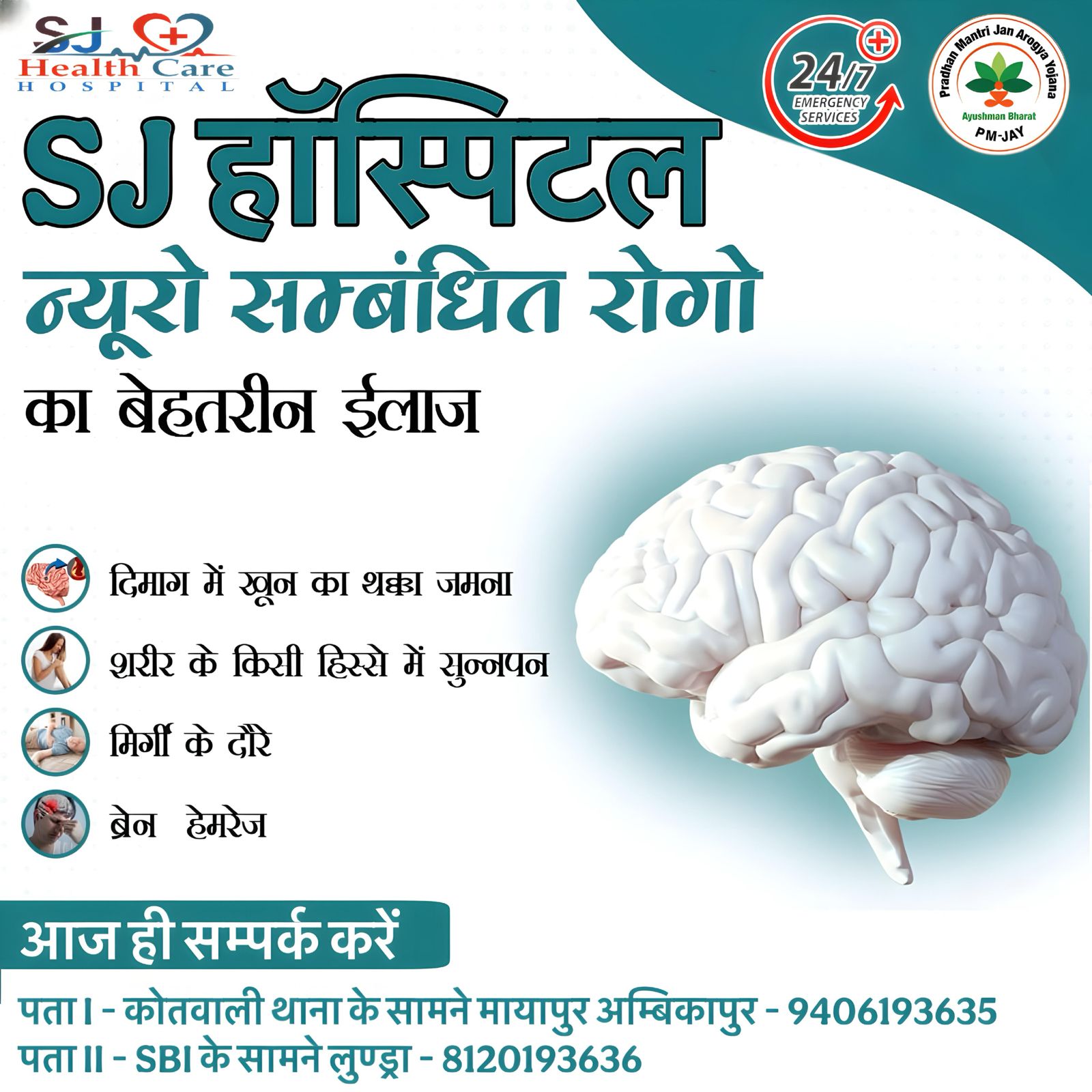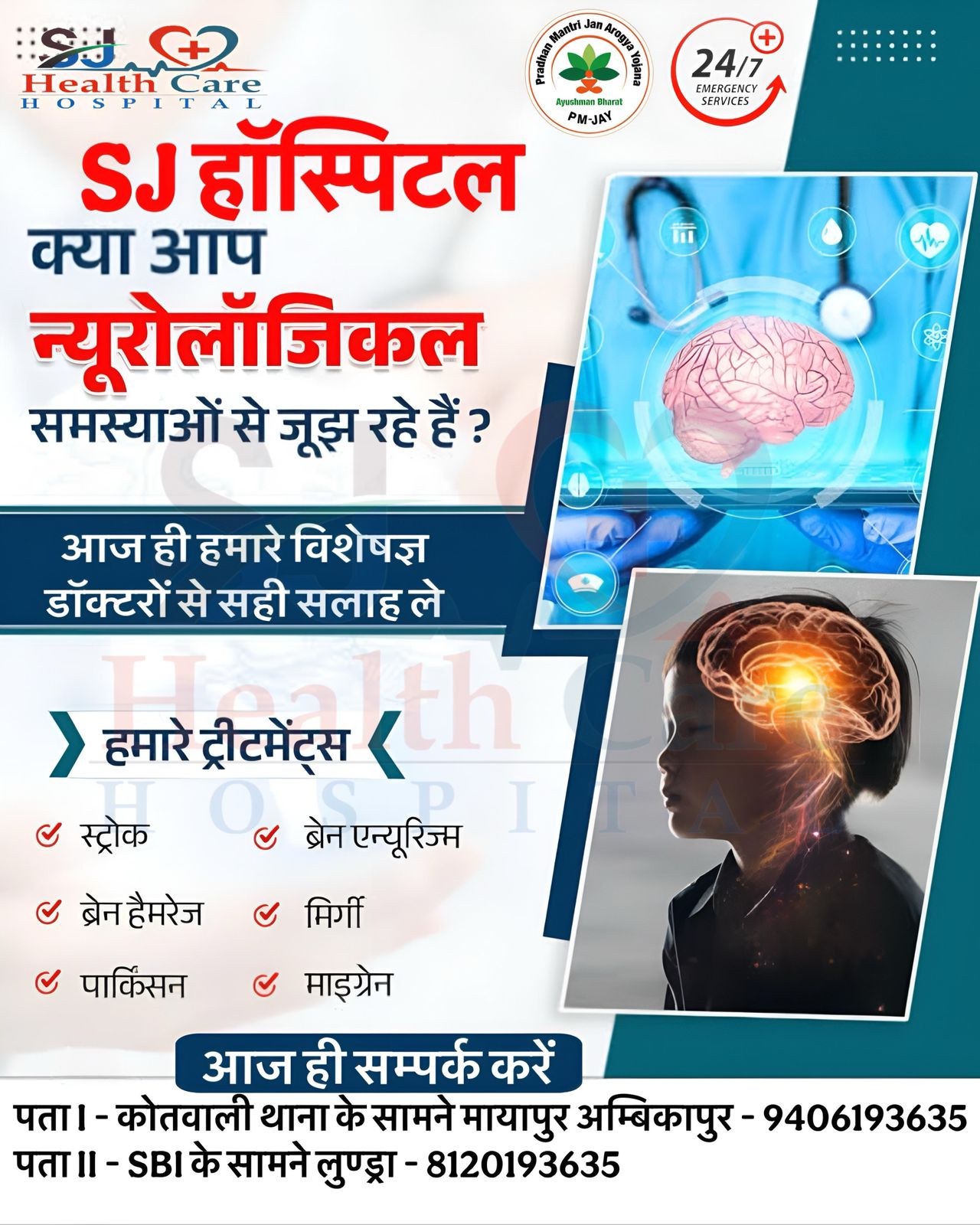क्या एनईपी हिंदी थोपने का प्रचार करता है? राज्य की भाषा नीति पर बहस जारी
जबकि कई राज्यों ने नई शिक्षा नीति की हिंदी थोपने के रूप में आलोचना की है, विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में यह मातृभाषा को जो महत्व देता है वह सही दिशा में एक कदम है।
क्या एनईपी हिंदी थोपने का प्रचार करता है? राज्य की भाषा नीति पर बहस जारी

जबकि कई राज्यों ने नई शिक्षा नीति की हिंदी थोपने के रूप में आलोचना की है, विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में यह मातृभाषा को जो महत्व देता है वह सही दिशा में एक कदम है।
पिछले हफ्ते, तमिलनाडु स्कूल शिक्षा आयुक्त ने दो भाषा नीति पर राज्य के रुख को दोहराते हुए एक प्रेस नोट जारी किया। “तमिल, जो मातृभाषा है, और वैश्विक-लिंक भाषा अंग्रेजी, दो-भाषा फार्मूले के अनुसार (राज्य में) प्रचलन में है।” यह उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें यह अनुमान लगाया गया था कि तमिलनाडु केंद्र द्वारा लूटी जा रही त्रि-भाषा नीति पर विचार कर सकता है। अब तक, तमिलनाडु त्रिभाषा फार्मूले का सबसे मुखर आलोचक बना हुआ है।
शिक्षा के माध्यम से “हिंदी थोपने” पर बहस 1966 में शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर कोठारी आयोग की रिपोर्ट के साथ शुरू हुई। तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों के लिए – सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक के लिए “हिंदी” का विरोध करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहा है। .
विवाद हाल ही में 31 मई 2019 को सार्वजनिक परामर्श के लिए नई शिक्षा नीति के मसौदे जारी होने के बाद फिर से सामने आया। केंद्र ने तब इसे संशोधित किया और स्पष्ट किया कि एनईपी 2020 में भाषा की कोई बाध्यता नहीं है।
29 जुलाई 2020 को एनईपी जारी होने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे “हिंदी और संस्कृत को थोपने” के प्रयास के रूप में वर्णित किया था। कर्नाटक ने भी औपचारिक विरोध दर्ज कराया, जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मसौदे को राज्यों पर क्रूर हमला बताया।
इस बीच, हिंदी भाषी राज्य भी छात्रों को अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन का विकल्प देने में विफल रहे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, अक्सर प्रदान की जाने वाली तीसरी भाषा का विकल्प संस्कृत है। NEP 2020 ने संस्कृत के मूल्य को त्रि-भाषा सूत्र में एक विकल्प के रूप में पेश करके उसे बहाल कर दिया। “इस प्रकार संस्कृत को स्कूली और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें त्रि-भाषा फॉर्मूला में एक विकल्प भी शामिल है।”
क्षेत्रीय स्कूल में पढ़ाती महिला
एक क्षेत्रीय स्कूल में अध्यापन करती एक महिला
“मैं यूपी से हूं और यूपी राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एक निजी स्कूल में पढ़ता हूं। केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर, हमें शायद ही कोई अन्य भारतीय भाषा सीखने को मिलती है, चाहे वह निजी या राज्य-सरकारी स्कूलों में हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए के छात्र बृजेश कुमार ने कहा, “कन्नड़, मलयालम या मराठी के लिए कई प्रशिक्षक नहीं हैं,” इसलिए अंततः “तीसरी भाषा के विकल्प के रूप में हमारे पास संस्कृत रह गई है।”
उदारवादी टिप्पणियों के बीच एनईपी के लिए कुछ समर्थन है। उनमें से प्रमुख हैं योगेंद्र यादव, जिन्होंने इसे “एक कदम आगे” कहा। सोशल मीडिया पर विभिन्न लेखों और वीडियो में, उन्होंने कहा है, “… एनईपी का मसौदा कहीं भी हिंदी-अराजकतावादी स्थिति नहीं लेता है, जबकि यह केवल त्रि-भाषा सूत्र को दोहराता है”। फिर भी, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हिंदी-बेल्ट वाले राज्य अन्य भारतीय भाषाओं को पढ़ाने से बचते हैं।
एक और बहस जो एनईपी ने पैदा की है वह है “शिक्षा के माध्यम” के आसपास। “नीति कहती है, कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, यह घरेलू भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, जहां भी संभव हो, घर/स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जारी रहेगा। इसके बाद सरकारी और निजी दोनों स्कूल होंगे।
कई छात्रों और शिक्षकों ने बताया है कि कक्षा 3 के बाद मातृभाषा के अलावा दो अतिरिक्त भाषाएं सीखने से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। साथ ही, मातृभाषा पर ध्यान देने से हाशिए की पृष्ठभूमि के कई छात्र अपने साथियों के मुकाबले वंचित स्थिति में रहेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने का खर्च उठा सकते हैं।
दिल्ली के शिक्षक और सेंट स्टीफंस कॉलेज के पूर्व छात्र अभिषेक कुमार ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में मुक्ति की क्षमता है। कुमार ने कहा, “अंग्रेजी सीखने के बाद, मुझे अब समाज में बेहतर स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि भारत में अंग्रेजी बोलने को महत्व दिया जाता है।”
कुमार ने बताया कि चूंकि वह हिंदी माध्यम की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। “मातृभाषा में सीखना ठीक है, लेकिन अंग्रेजी एक आवश्यकता है। मुझे जीवन में आत्मविश्वासी बनने के लिए अपने भाषा कौशल के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा।”
भारतीय माता-पिता यह पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे स्थानीय स्कूलों में पढ़ते हैं। हालांकि निजी स्कूलों में नामांकन 2018 में 32.5 प्रतिशत से घटकर 2020 में 28.8 प्रतिशत हो गया, जो 6-14 वर्ष की आयु के बीच था, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश ने “अंग्रेजी माध्यम” टैग के कारण निजी स्कूलों को चुना। “अंग्रेजी एक आवश्यकता है, और केवल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ही इसे बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने वाले स्कूलों का रखरखाव अक्सर खराब होता है, ”5 साल के लड़के की मां आकृति वर्मा कहती हैं।
दूसरों का तर्क है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। लद्दाख के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट के संस्थापक सोनम वांगचुक, जिन्होंने खुद नौ साल की उम्र तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की थी, ने ट्विटर पर लिखा था “मुझे संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम दुनिया को समझने में अवधारणाओं को समझने की कुंजी है, यहां तक कि अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं को सीखने की भी कुंजी है।”
एनईपी में यह विचार अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया जैसी अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है, जिन्होंने बाद में जीवन में अंग्रेजी सीखी, और मातृभाषा में पढ़ाने के विचार का समर्थन करते हैं क्योंकि यह छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
मातृभाषा में पढ़ाना अपने आप में कोई नया विचार नहीं है। अनुच्छेद 350A स्पष्ट रूप से कहता है कि एक राज्य को मातृभाषा में सीखने की सुविधा देनी चाहिए। “भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के भीतर प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा।” शिक्षा का अधिकार, 2009, ने भी प्रतिध्वनित किया कि मातृभाषा को “शिक्षा के माध्यम” के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
हालांकि, आदिवासी या स्थानीय भाषाओं को जानने वाले शिक्षकों की कमी है। कुछ जनजातियों के सदस्य स्वयं अपनी भाषा भूल गए हैं, उदाहरण के लिए, कमजोर जनजाति सहरिया। एक और बड़ी चुनौती जो अल्पसंख्यक भाषाओं को वंचित स्थिति में डालती है, वह यह है कि मातृभाषा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक भाषा को 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, इसे अल्पसंख्यक भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “समस्या कार्यान्वयन के साथ है। राज्य अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता देने के लिए अनिच्छुक हैं