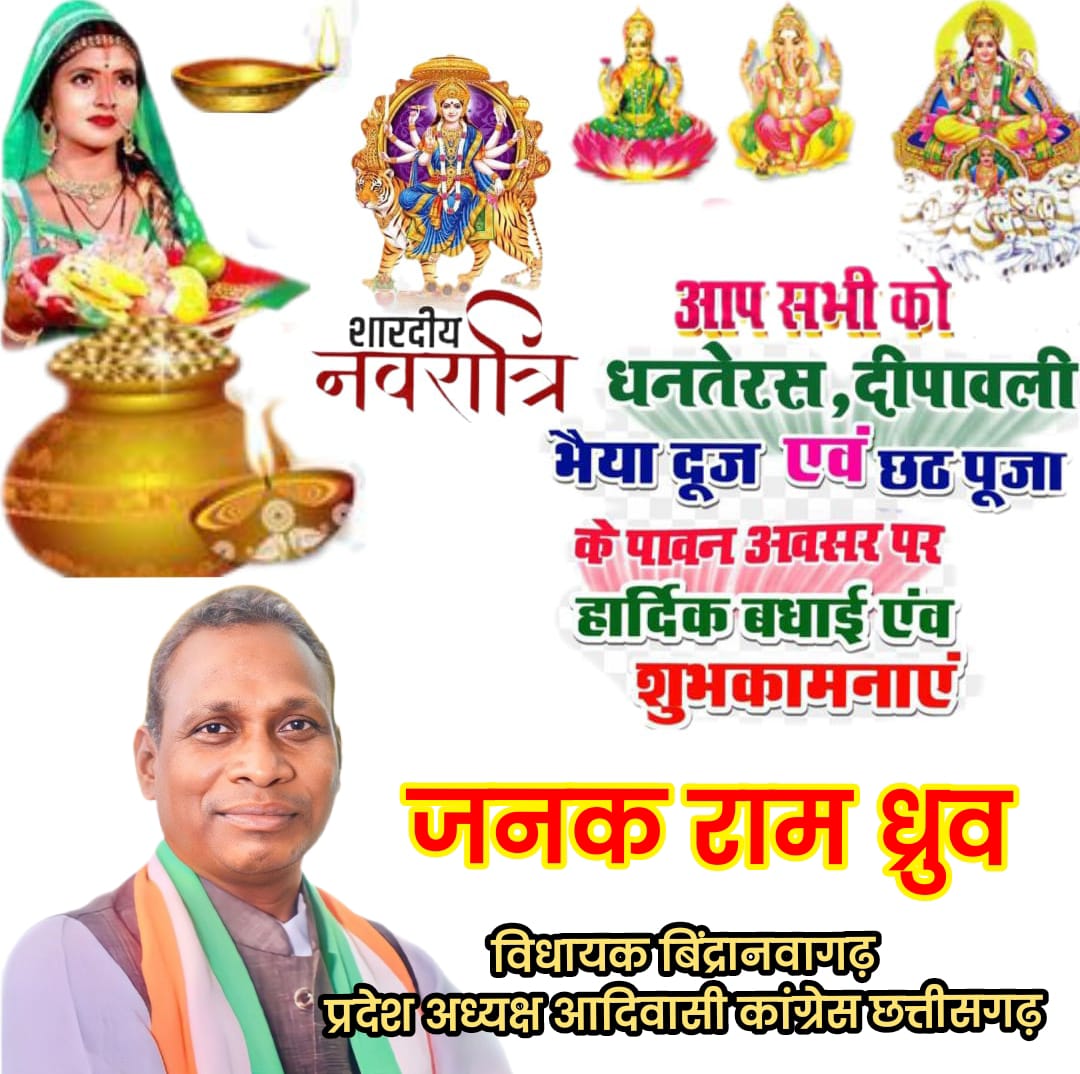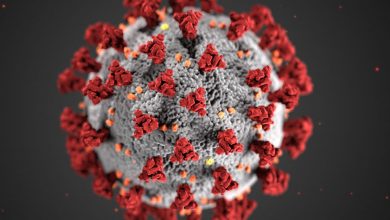भगवा चुनौती में हिंदी साहित्य कैसे विफल हुआ।
भगवा चुनौती में हिंदी साहित्य कैसे विफल हुआ
प्रमुख लेखकों की चुप्पी से पता चलता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र का दक्षिणपंथी बदलाव अपरिहार्य था।
उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम हमें हिंदी भाषी क्षेत्र की साहित्यिक संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं? जाहिर है कि लोगों ने भगवा विचारधारा को अपना लिया है, लेकिन क्या हिंदी साहित्यिक प्रतिष्ठान-जिस पर कभी वामपंथियों का दबदबा था-आधार बदल गया है? हिंदी साहित्य का राजनीतिक लेखन, जिसके माध्यम से इसने कभी सत्ताधारी शासन का बड़ा प्रतिरोध किया था, आज कहां खड़ा है? हिंदी जगत में चल रहा एक तूफान इन सवालों के कुछ सुराग पेश कर सकता है जो भाषा और उसके साहित्य के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए इसके जलग्रहण क्षेत्र की राजनीति को परिभाषित कर सकते हैं।
चुनाव परिणाम से कुछ दिन पहले, हिंदी के सबसे प्रिय और मितभाषी लेखकों में से एक विनोद कुमार शुक्ला (85) ने एक लघु वीडियो क्लिप जारी करके अपने पाठकों को चौंका दिया, जिसमें उन्होंने अपने प्रकाशकों से अपनी पुस्तकों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, प्रकाशकों ने उन्हें देय रॉयल्टी का भुगतान नहीं करके और ऐसा नहीं करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करके धोखा दिया। दिल को झकझोर देने वाले इस वीडियो ने लोगों में खूब गुस्सा निकाला। उनका अकेला उदाहरण नहीं था। अधिकांश हिंदी लेखक अक्सर अपने प्रकाशकों द्वारा ठगे जाने की शिकायत करते हैं। और फिर भी, उनके समर्थन में एक अभियान शुरू होने के बाद, प्रगतिशील लोगों सहित बड़ी संख्या में हिंदी लेखकों ने प्रकाशकों का साथ दिया। इन लेखकों ने शुक्ला और उनके मुद्दे को उठाने वालों को भी दोषी ठहराया।उन्होंने बूढ़े लेखक को क्यों छोड़ दिया? कथा लेखक चंदन पांडे शुक्ल प्रकरण और यूपी में चुनावी परिणामों के बीच एक व्यावहारिक संबंध बनाते हैं। “जब एक लेखक और प्रकाशकों के बीच की प्रतियोगिता में, अधिकांश बुद्धिजीवी ताकतवर का पक्ष ले रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी शक्तिशाली शासकों को त्याग देगा?” वह पूछता है। तुलना तीक्ष्ण है।“हिंदी साहित्य जगत प्रकाशक पर केन्द्रित है। वरिष्ठ लेखक असगर वजाहत, जो एक वामपंथी संगठन के पदाधिकारी भी हैं, ने शुक्ला द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद अपने प्रकाशक से अपनी किताबें वापस लेने की घोषणा की। लेकिन संगठन उनके समर्थन में नहीं आया, ”लेखक प्रभात रंजन कहते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, या तो हिंदी साहित्यकारों के एक बड़े हिस्से ने चुपचाप हिंदुत्व खेमे में अपना नया घर बना लिया है, या अब उनके पास राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए उपकरण या सहनशक्ति और इरादा नहीं है। गहरी खुदाई करें और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी विफलता शायद अपरिहार्य थी। सबसे पहले, अधिकांश लेखक हिंदुत्व की भावना का पर्याप्त रूप से विरोध नहीं कर सके क्योंकि यह पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है। दूसरा, कड़वी जातिवाद और स्त्री द्वेष से चिह्नित हिंदी साहित्यकार शायद भगवा के धार्मिक आकर्षण को चुनौती नहीं दे सकते थे। तीसरा, डिजिटल क्रांति ने लोकप्रिय लेखन का जश्न मनाया और पढ़ने की संस्कृति को मौलिक रूप से बदल दिया। और चौथा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1980 के दशक के मंदिर आंदोलन के दौरान हिंदी मीडिया बहुत पहले दक्षिणपंथी हो गया था।हिंदी लेखकों द्वारा हिंदुत्व को कमजोर चुनौती के बारे में बोलते हुए, वरिष्ठ वामपंथी लेखक अखिलेश कहते हैं: “चेतना के स्तर पर सांप्रदायिकता का विरोध है, लेकिन यह साहित्यिक कार्यों में परिलक्षित नहीं होता है। कई कवियों ने 6 दिसंबर के बारे में कविता लिखी, जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। तब नरेंद्र मोदी की पीएम के रूप में नियुक्ति को चिह्नित करने वाली कविताओं की एक पूरी श्रृंखला थी। लेकिन इनमें से अधिकांश कविताएँ एक निश्चित प्रतिबद्धता के लिए लिखी गई लगती थीं, और आंतरिक उथल-पुथल को नहीं दर्शाती थीं।”प्रभावशाली साहित्यिक पत्रिका तद्भव का संपादन करने वाले अखिलेश ने रेखांकित किया कि हाल के दशकों में अधिकांश राजनीतिक लेखन एक थोपी गई “प्रतिबद्धता” से बाहर लिखा गया था, एक भावना “चूंकि एक घटना थी, मुझे इस पर लिखना पड़ा”। ये “प्रतिबद्ध” लेखन संभवतः मंदिर आंदोलन के जोशीले एजेंडे का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रतिबद्धता वास्तविक क्यों नहीं थी? शायद अधिकांश लेखकों ने भाजपा की राजनीति के लिए एक नरम तत्व रखा। हो सकता है कि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित न किया हो, लेकिन उन्होंने बाड़ को बहुत पहले ही बदल दिया था, और इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ जुड़ाव पर्याप्त गंभीर नहीं था। अखिलेश कहते हैं, ”हिंदी साहित्य में साम्प्रदायिकता की सरल व्याख्या है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक जटिल परिघटना है.”फिर निहित कुप्रथा और जातिवाद हैं। प्रगतिशील मोर्चे के अगुवा स्वर्गीय नामवर सिंह जैसे व्यक्ति ने भी अपने ठाकुर मूल को गर्व से दिखाया। यदि वामपंथी प्रतिष्ठान का एक प्रमुख व्यक्ति किसी विशेष जाति को बढ़ावा दे रहा था, तो उसके पास भाजपा के ठाकुरवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत कम नैतिक आधार था, जो दशकों बाद यूपी में आने वाला था। युवा लेखिका अनु शक्ति सिंह साथी लेखकों की सेक्सिस्ट टिप्पणियों का सामना करने का अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हैं। “बड़े पैमाने पर अनुसरण करने वाले लेखक महिलाओं, अन्य धर्मों और जातियों के प्रति अपनी घृणा को खुले तौर पर प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। जब साहित्यिक प्रतिष्ठान ही खुद से समझौता कर रहा है, तो आप उनके लेखन से क्या उम्मीद कर सकते हैं?”
यह सुनिश्चित करने के लिए, अधिकांश लेखक अपने भीतर एक क्रूर द्विभाजन रखते हैं। उनका जीवन उन्हीं आदर्शों का खंडन करता है जिनकी वे अपने लेखन में वकालत करते हैं। हालाँकि, जो विद्वता कभी केवल उनके आंतरिक सर्कल के लिए जानी जाती थी, वह अब डिजिटल युग में सार्वजनिक प्रदर्शन पर है। समर्पित पाठक लेखक की एक आदर्श छवि रखते हैं, जो उनके वास्तविक जीवन के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लेखक के बारे में एक रहस्य, एक आभा बनाए रखने में मदद करता है। सोशल मीडिया ने लेखकों को आभा से दूर कर दिया है। वे अब नग्न खड़े हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने और अपनी किताबें बेचने के लिए बेहूदा हरकतें और अश्लील स्टंट करते हैं। साहित्य से मोहभंग होना लाजमी है। “ऐसे लेखक कैसे जनता को प्रभावित कर सकते हैं और बौद्धिक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं?” सिंह से पूछता है।
वेब पत्रिका हिंदवी के युवा संपादक अविनाश मिश्रा भी उनकी आलोचना में ज़बरदस्त हैं. “हिंदी साहित्य जगत की अंतर्निहित संरचना शुरू से ही गहरी राजनीतिक रही है। लेकिन हिंदी का सार्वजनिक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से जातिवादी, सांप्रदायिक और हिंसक है। इस विडम्बना के कारण हिन्दी का लेखक सामाजिक आधार नहीं बना पाता।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पैदा हुआ, आधुनिक हिंदी साहित्य दृढ़ता से आदर्शवादी और स्थापना विरोधी था, और उथल-पुथल के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई। हिंदी लेखक सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं के मित्र थे और उन्होंने राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद की। अखिलेश ने नोट किया कि आजादी के बाद राजनीतिक लेखन की प्रकृति बदल गई। वे कहते हैं, “स्वतंत्रता के बाद के हिंदी साहित्य में नेहरूवादी मूल्यों की छाप थी, और इस तरह समकालीन राजनीति की एक महत्वपूर्ण आलोचना नहीं कर सका,” वे कहते हैं, और फिर नेहरू के बाद के राजनीतिक लेखन में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जब नेहरूवादी युग से मोहभंग हुआ, तो अधिकांश लेखकों ने क्षय की आलोचना करने के बजाय, ऐसे व्यक्तियों को चित्रित किया, जो अपने आप में वापस आ गए थे। वे कहते हैं, “राजनीति का विरोध करने के बजाय, नेहरूवादी युग के बाद के साहित्य के नायक एकाकी और उदास हो गए।”
हिंदी में जितने छोटे राजनीतिक लेखन थे, उनमें से अधिकांश में सत्ता संरचनाओं की गहरी समझ और आलोचना का अभाव था। अखिलेश कहते हैं, ”हमारे लेखन में पीड़ितों का पर्याप्त लेखा-जोखा है, लेकिन सत्ता के ढांचे की वास्तविकता और जटिलताएं मुश्किल से ही हैं.” वह कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के प्रसिद्ध छंद “तोडन होंगे मठ” का हवाला देते हैं, और पूछते हैं: “प्रतिरोध है, लेकिन गढ़ क्या है, यह कैसे संचालित होता है, इसके किलेबंदी क्या हैं, शोषण के तरीके क्या हैं? शक्ति संरचना की आलोचना ज्यादातर अनुपस्थित है। सबसे अच्छे रूप में, यह एक नीरस चित्रण के रूप में आता है, न कि एक व्यावहारिक आलोचना के रूप में।” अखिलेश इस बात को रेखांकित करते हैं कि “वर्ग संघर्ष के नाम पर लिखी गई कल्पना की कई कृतियाँ एक नकली क्रांति और नकली आदर्शवाद द्वारा चिह्नित की गई थीं। इस फिक्शन में उत्साह ज्यादा था लेकिन गहराई कम थी।” इस तरह की जाली प्रगतिशील भावना संभवतः जनता को प्रभावित नहीं कर सकती थी, जिन्होंने भगवा विकल्प को कम से कम आश्वस्त और भावुक पाया।
इस बीच वैश्वीकरण से चुनौती आई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब से हिंदी एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उभरी, तब से भाषा पर राष्ट्र की ऐतिहासिक विरासत को आकार देने की जिम्मेदारी थी। इसकी लोकप्रिय कथा साहित्य की परंपरा रही है, लेकिन इसे साहित्यिक प्रतिष्ठान से बहुत कम सम्मान मिला। पिछले दशक में एक आश्चर्यजनक उलटफेर देखा गया है, क्योंकि प्रमुख प्रकाशकों ने लोकप्रिय लेखन को गोद लिया है। क्राइम-थ्रिलर लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक, जिनके उपन्यास दशकों से छोटे-छोटे प्रकाशकों द्वारा धुंधले कागज पर छपे थे, अब खुद को प्रमुख प्रकाशकों के रूप में पाते हैं। जब अधिकांश लेखकों को मामूली रॉयल्टी मिलती है, तो लोकप्रिय कविता-मास्टर कुमार विश्वास को हाल ही में आठ अंकों की अग्रिम रॉयल्टी मिली, जो शायद अब तक की सबसे अधिक है। हिंदी में इससे पहले कभी भी लोकप्रिय ग्रंथों को गंभीर साहित्य को बदनाम करने की हद तक नहीं मनाया गया। “पिछले तीन दशकों में, हिंदी समुदाय ने बड़ी गति से गैर-बौद्धिकीकरण किया है। पिछले सात वर्षों में जो उपन्यास आए हैं, उनमें बेकार रोमांस और सस्ते रोमांच की बाढ़ आ गई है। अविनाश मिश्रा कहते हैं, ये काम उनके आसपास सामने आ रहे संकट की जांच नहीं करते हैं।
लोकलुभावनवाद की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बुद्धिजीवी (बौद्धिक) शब्द को अब अक्सर अपमानजनक उपयोग के रूप में फेंक दिया जाता है। बुद्धिजीवियों के खिलाफ भाजपा के अभियान को दोष दिया जा सकता है, लेकिन कई हिंदी लेखकों ने भी अपनी जमीन खो दी। “राजनीतिक लेखन की विश्वसनीयता कम हो गई है। दक्षिणपंथी राजनीतिक लेखन की कभी कोई विश्वसनीयता नहीं रही; वामपंथी लेखन की विश्वसनीयता अब कम हो गई है। बौद्धिक समुदाय को अब उन्हीं लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था, ”प्रभात रंजन कहते हैं।
परिवर्तन की नींव शायद 1980 के दशक में हिंदी मीडिया द्वारा राम मंदिर आंदोलन की कवरेज के दौरान रखी गई थी। उस समय तक, हिंदी क्षेत्र में धर्मयुग, सप्ताहिक हिंदुस्तान और दिनमान जैसे गौरवशाली प्रकाशन थे, जिनका नेतृत्व बड़े-बड़े लेखकों ने किया था, जिन्हें अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त थी। साहित्यिक और मीडिया प्रकाशनों ने एक-दूसरे का भरपूर पोषण किया। मंदिर आंदोलन, जो उस समय हुआ था जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण को गले लगा रही थी, हिंदी मीडिया ने एक निर्णायक मोड़ लिया। जबकि अंग्रेजी प्रकाशनों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को “राष्ट्रीय शर्म” कहा, कई हिंदी दैनिक समाचार पत्रों की कवरेज जश्न मनाने वाली थी। चलन तेज हो गया है। पिछले सात वर्षों के हिंदी मीडिया में सत्ता से सच बोलने वाले विरोधियों की आवाज आसानी से नहीं मिलती। जब कई अंग्रेजी दैनिकों ने 2018 में #MeToo आंदोलन का समर्थन करने वाले लेख प्रकाशित किए, तो प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों ने विरोध करने वाली महिलाओं पर सवाल उठाया और यहां तक कि आरोपी के संस्करण पर भरोसा किया।
बड़े पैमाने पर प्रसार और विज्ञापन राजस्व के बावजूद, हिंदी प्रिंट मीडिया ने मूल रिपोर्टिंग में बहुत कम निवेश किया है, खुशी से वायर एजेंसियों से प्रतियों को फिर से प्रकाशित किया है या अंग्रेजी में अपनी बहन प्रकाशनों से कहानियों का अनुवाद किया है। कुछ 530 मिलियन लोगों की भाषा, कुछ 10 राज्यों की पहली भाषा, एक ऐसी भाषा जो “राष्ट्रीय भाषा” बनने की इच्छा रखती है, ने अपने बौद्धिक नेतृत्व को सौंप दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शानदार उत्पादों के बीच प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी कहते हैं, “इलाहाबाद ‘हिंदी साहित्य का गढ़ (हिंदी साहित्य का किला)’ था, निश्चित रूप से लगभग 1900 से लेकर 1980 तक – इसके बाद गौरव चला गया।” वह इलाहाबाद के कई लेखकों को सूचीबद्ध करता है “जो बड़े चरागाहों के लिए चले गए, जिन्हें आने वाली चीजों के शगुन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए था”।
भाजपा के लिए कोई भी राजनीतिक चुनौती हृदयभूमि से आनी चाहिए क्योंकि हिंदी पट्टी इतनी मजबूत है कि अन्य राज्यों द्वारा किए गए किसी भी प्रतिरोध को नीचे गिरा दिया जा सकता है। और हिंदी साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के बिना हिंदी भाषी क्षेत्र में किसी भी आंदोलन के आने की संभावना नहीं है। “यूपी चुनाव के नतीजे बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण का संकेत देते हैं। बीमारी सांस्कृतिक और सामाजिक पतन है, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ”चंदन पांडे कहते हैं।
हिंदी दुनिया शायद अब तक के सबसे बड़े अस्तित्व के सवाल का सामना कर रही है। छह दशक पहले, कवि के सामने चुनौती “सभी मठों (गढ़ों) को ध्वस्त करने” की थी। अपनी ईमानदारी खो चुके सभी गढ़ आज बुरी तरह जर्जर हो चुके हैं। हिंदी एक नए घर का इंतजार कर रही है।
(यह प्रिंट संस्करण में “राइट चॉइस” के रूप में दिखाई दिया)
आपने इस युद्ध की शुरुआत की। यू कैन स्टॉप दिस वॉर’: श्वार्जनेगर टू पुतिन