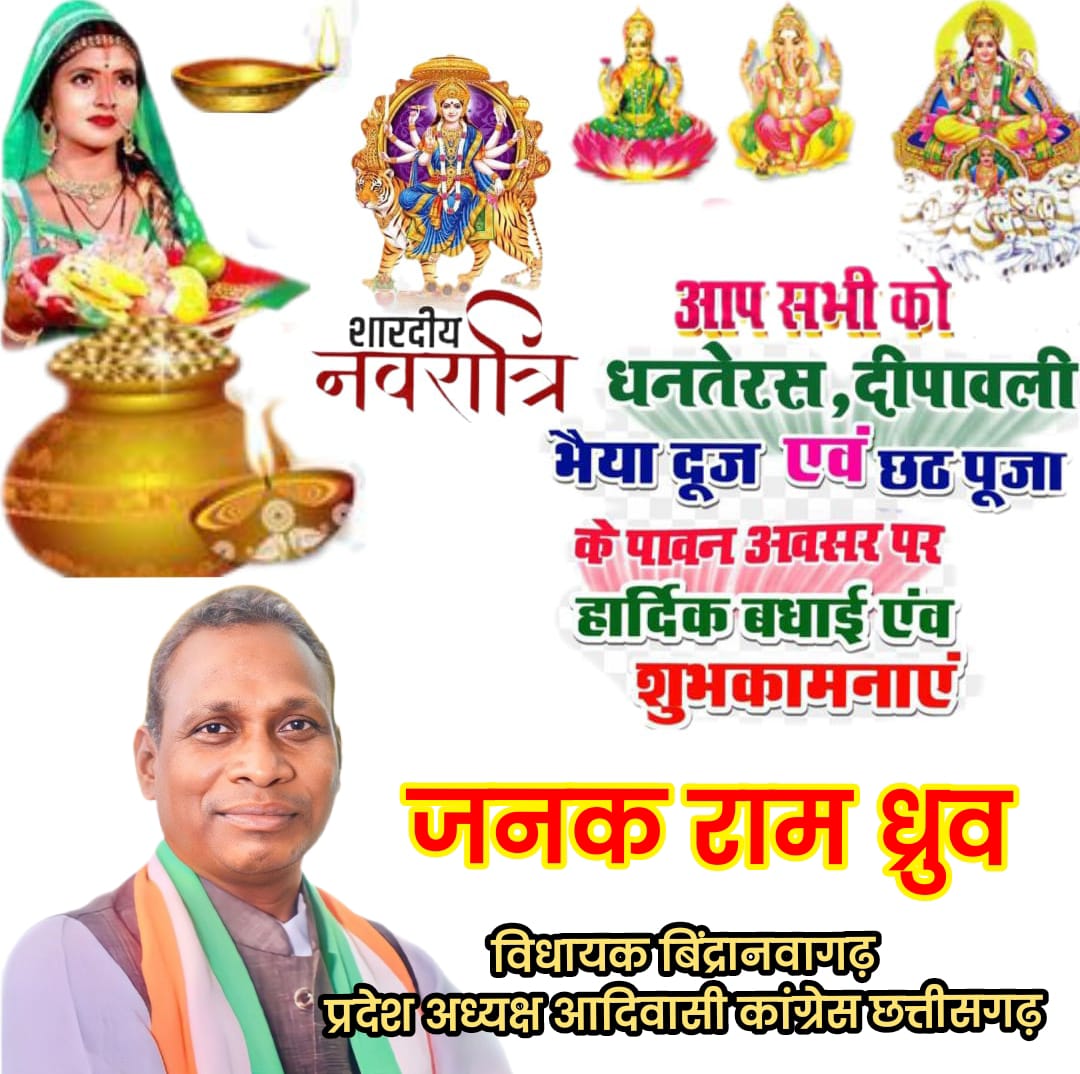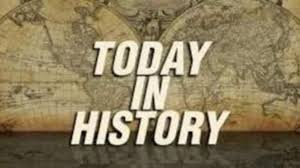भाषाओं के समूह ने हिंदी बोलने वालों की संख्या को कैसे बढ़ाया
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 53 करोड़ कथित हिंदी भाषियों में से 12 करोड़ वास्तव में बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो अपनी मान्यता की प्रतीक्षा कर रही हैं।
हिंदी ने पांच दशकों में बोलने वालों की संख्या में असाधारण वृद्धि दर्ज की- 1961 में भारत की आबादी का 30.39 प्रतिशत (13.34 करोड़) से 2011 में 43.63 प्रतिशत (52.83 करोड़) तक। लेकिन यह उचित मान्यता से वंचित करने की कीमत पर आया था। इसके साथ समानता रखने वाली अन्य भाषाओं के लिए। जैसा कि जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है, यह उधार की महिमा में आधार बनाने का मामला है।
कुरमाली और मगही या मगधी के मामलों पर विचार करें, जिन्हें 1971 की जनगणना रिपोर्ट के बाद से हिंदी के तहत मातृभाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
देश की 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करने वाले भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अपनी मातृभाषा कुर्माली को शामिल करने की मांग की। जनवरी 2021 में, कुर्मी-महतों ने इस मांग के लिए दबाव बनाने के लिए दक्षिण-पश्चिम पश्चिम बंगाल के चार जिलों में लगभग 50 स्थानों पर सड़क जाम भी किया।
उनकी मांग नई नहीं थी। 2009 में, दूसरी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने संसद को सूचित किया कि कुरमाली सहित 38 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष लंबित थी। मई 2015 में जमशेदपुर से लोकसभा सदस्य विद्युत बरन महतो ने संसद में भी यही मांग उठाई।
मान्यता की प्रतीक्षा कर रही इन 38 भाषाओं में से 12-कुरमाली सहित- 12.2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली (2011) को 1971 से हिंदी के तहत मातृभाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक प्रस्ताव है जिसका इन भाषाओं के बोलने वाले विरोध करते हैं।
इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या में वृद्धि पर ही हिंदी के विकास के दावे आधारित हैं।
इसके विपरीत, यदि हम वास्तव में अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वाले लोगों की हिस्सेदारी को देखें, तो यह 1961 में 28.02 प्रतिशत (12.3 करोड़) से घटकर 2011 में 26.61 प्रतिशत (32.22 करोड़) हो गई है। इस अवधि के दौरान, जनसंख्या भारत में 2.75 गुना की वृद्धि हुई, जबकि हिंदी बोलने वालों के रूप में अपनी पहचान बनाने वालों की संख्या में 2.61 गुना की वृद्धि हुई।
कुर्माली कुर्मी-महतो की मातृभाषा है – बिहार के कुर्मियों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए – जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ट्राइजंक्शन में रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 425,920 कुरमाली बोलने वालों में से 3,06,756 पश्चिम बंगाल में और 1,12,916 ओडिशा में रहते थे। भाषा बंगाली, हिंदी, उड़िया और संताली से प्रभावित है लेकिन अलग बनी हुई है।
1898 और 1927 के बीच भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के प्रकाशन की अगुवाई करने वाले एंग्लो-आयरिश भाषाविद् जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कुरमाली को “पश्चिमी बंगाली का एक रूप” और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, खंड V – भाग I के रूप में वर्णित किया। बंगाली में, कभी कैथी में, और कभी उड़िया लिपि में। तपती घोष ने भारत की जनगणना प्रकाशनों में भाषा के अपने परिचय में लिखा है कि “बंगाली भाषा का प्रभाव उनके दैनिक संचार में पाए जाने वाले हिंदी के समानांतर चलता है जो काफी हद तक बंगाली पारिस्थितिकी से प्रभावित होता है।” यह देवनागरी लिपि में भी लिखा गया है।
ब्रिटिश प्रशासन ने बिहार की अन्य भाषाओं (ज्यादातर दक्षिण बिहार में छोटानागपुर, अब झारखंड) के साथ व्याकरणिक समानता के कारण भाषाओं के बिहारी समूह के तहत भाषा को सूचीबद्ध किया था और 1961 की जनगणना ने इसे बनाए रखा। हालाँकि, 1971 की जनगणना में हिंदी के तहत सूचीबद्ध सभी भाषाओं को पहले बिहारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, कुरमाली, या कुरमाली थार, हिंदी के तहत एक मातृभाषा बन गई।
सदरी, छोटानागपुर क्षेत्र की एक अन्य भाषा, 2011 में 51.27 लाख लोगों द्वारा बोली जाती थी, इसे सदन, गवरी और नागपुरी या नागपुरिया के रूप में भी जाना जाता है, (अंतिम दो नाम छोटानागपुर का जिक्र करते हैं और महाराष्ट्र के नागपुर नहीं)। भारत की 2001 की जनगणना से पता चला है कि भारत में लगभग 32.76 लाख सदरी/नागपुरी बोलने वाले, आधे झारखंड में रहते थे और शेष पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए थे।
ICANN (इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स) दस्तावेज़ के अनुसार, सदरी “प्रमुख क्षेत्रीय आदिवासी प्रभाव के साथ ओडिया और हिंदी भाषा का मिश्रण है”। भाषाविद् टोबी एंडरसन द्वारा संकलित और यूएस-आधारित गैर-लाभकारी एसआईएल इंटरनेशनल द्वारा 2020 में प्रकाशित सदरी-हिंदी शब्दकोश में कहा गया है कि अन्य भाषाओं के साथ सादरी की “व्याख्यात्मक समानता” में हिंदी के साथ 58-71 प्रतिशत, ओडिया के साथ 47-54 प्रतिशत शामिल हैं। और बंगाली के साथ 45-61 प्रतिशत। इसमें कहा गया है कि बंगाली और देवनागरी दोनों लिपियों का उपयोग करके साहित्य और रेडियो कार्यक्रम विकसित किए गए हैं।
हालाँकि, 1971 की जनगणना के अधिकारियों ने इसे हिंदी के तहत जोड़ना सबसे अच्छा समझा, वह भाषा जिसे केंद्र सरकार दूसरों पर पसंद करती थी।
एक विकास के क्रॉनिकल की भविष्यवाणी की गई
1971 की जनगणना ने भारत की भाषा नीति, या भाषा की राजनीति के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, चाहे वह किसी भी तरह से वर्णित हो। यह तीन साल बाद आया जब भारत ने हिंदी समर्थक नीति को लागू करने की दिशा में पहला बड़ा कदम देखा- जनवरी 1968 में, संसद ने केंद्र सरकार के सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने पर जोर देने का संकल्प लिया। इस कदम को संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन मिला।
संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि “संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, (और) इसे विकसित करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। …”, जबकि अनुच्छेद 344 ने “संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग” के प्रावधान किए।
हालाँकि, दो चेतावनियाँ थीं। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि अन्य अनुसूचित भाषाओं के साथ “हस्तक्षेप किए बिना” आत्मसात करके हिंदी की समृद्धि को सुरक्षित किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि अधिकारी