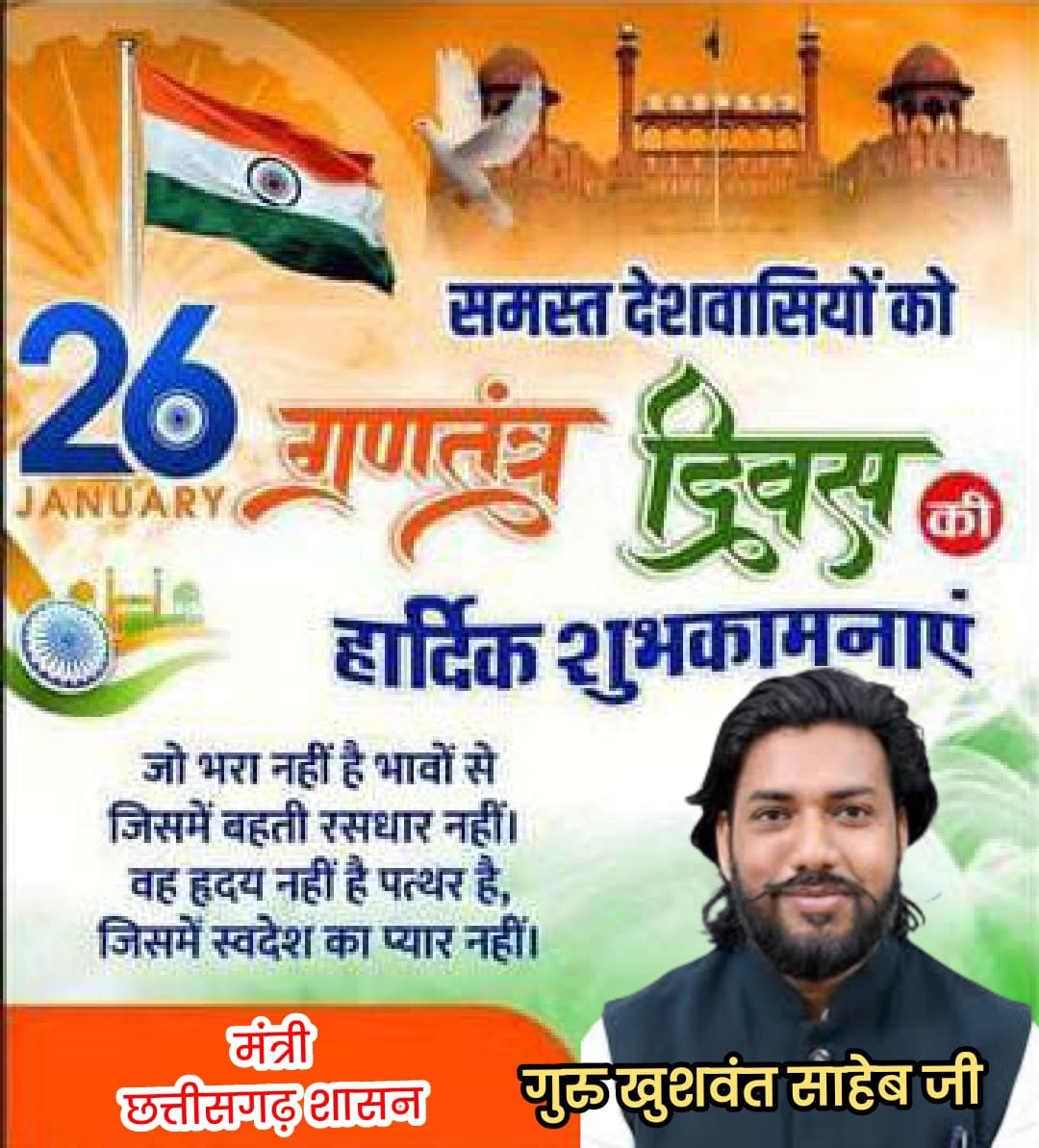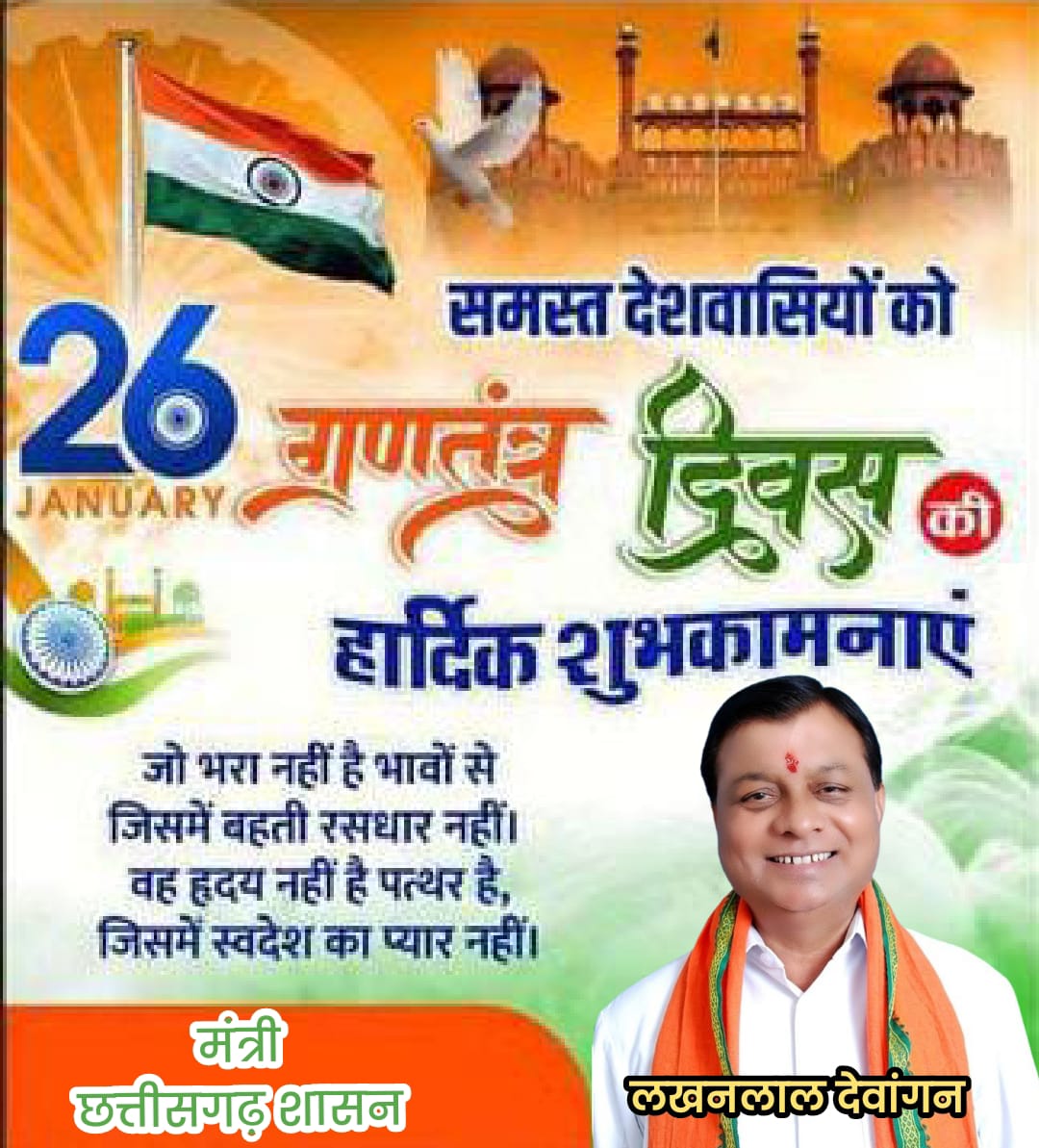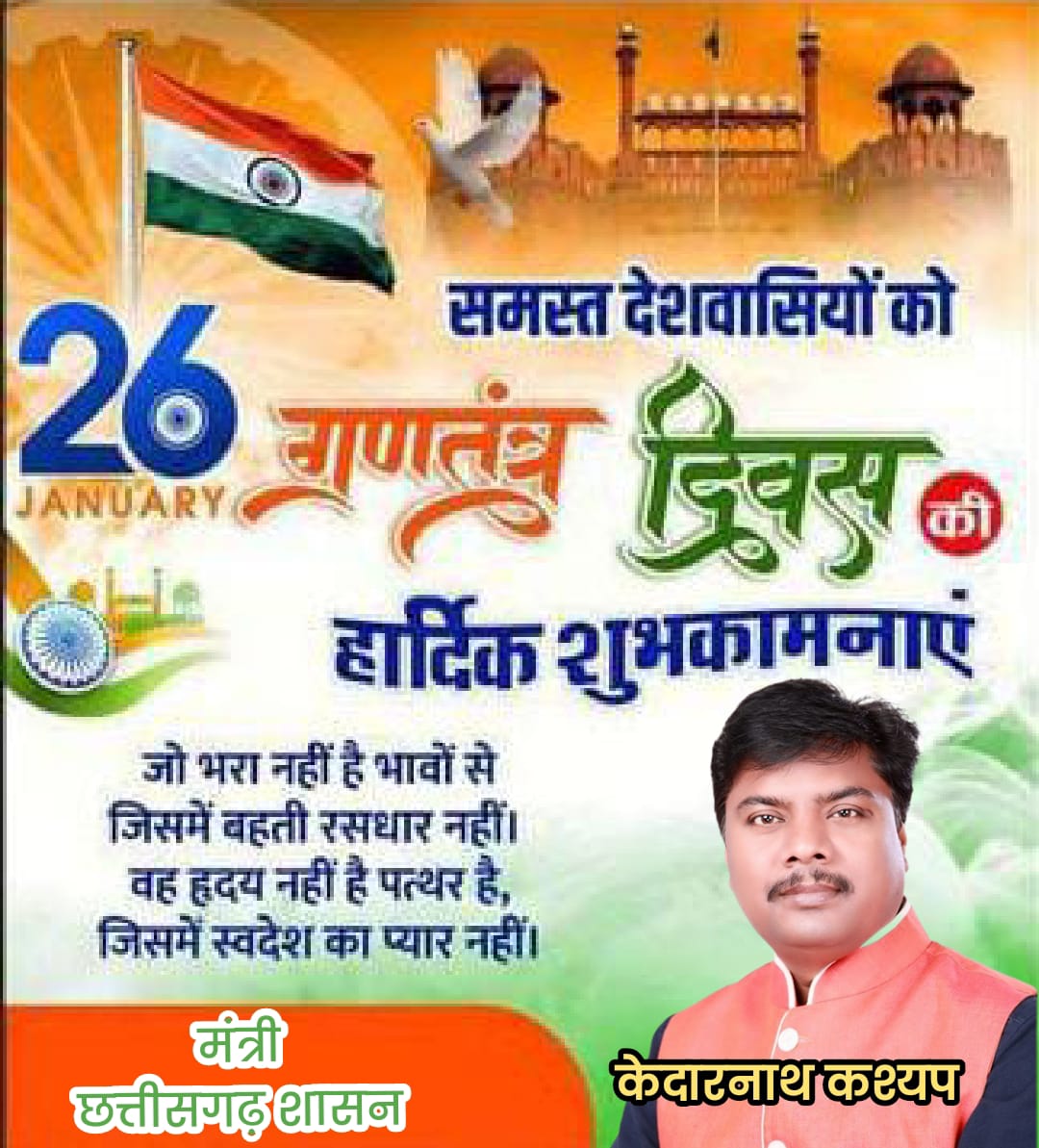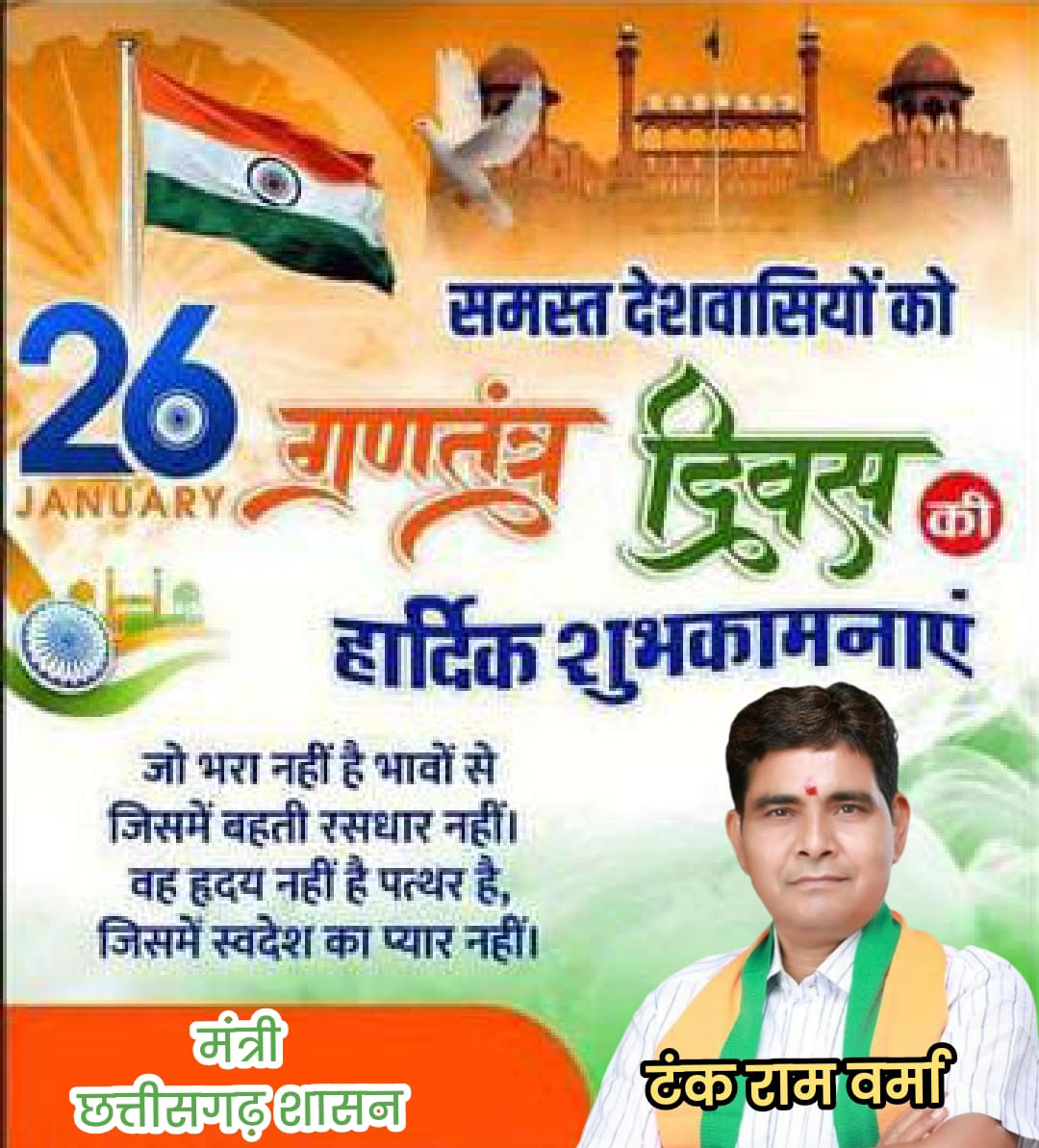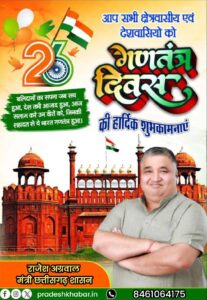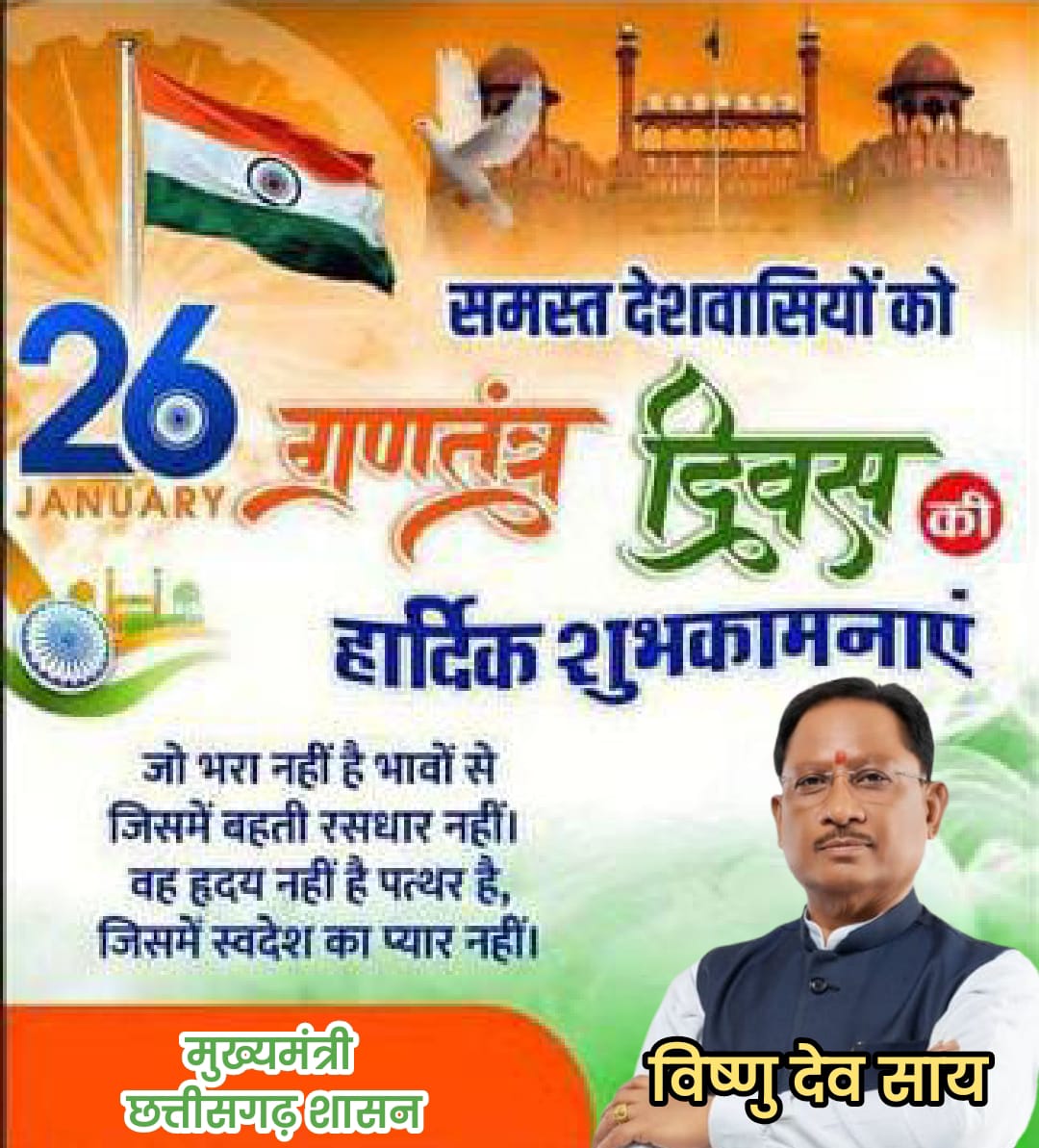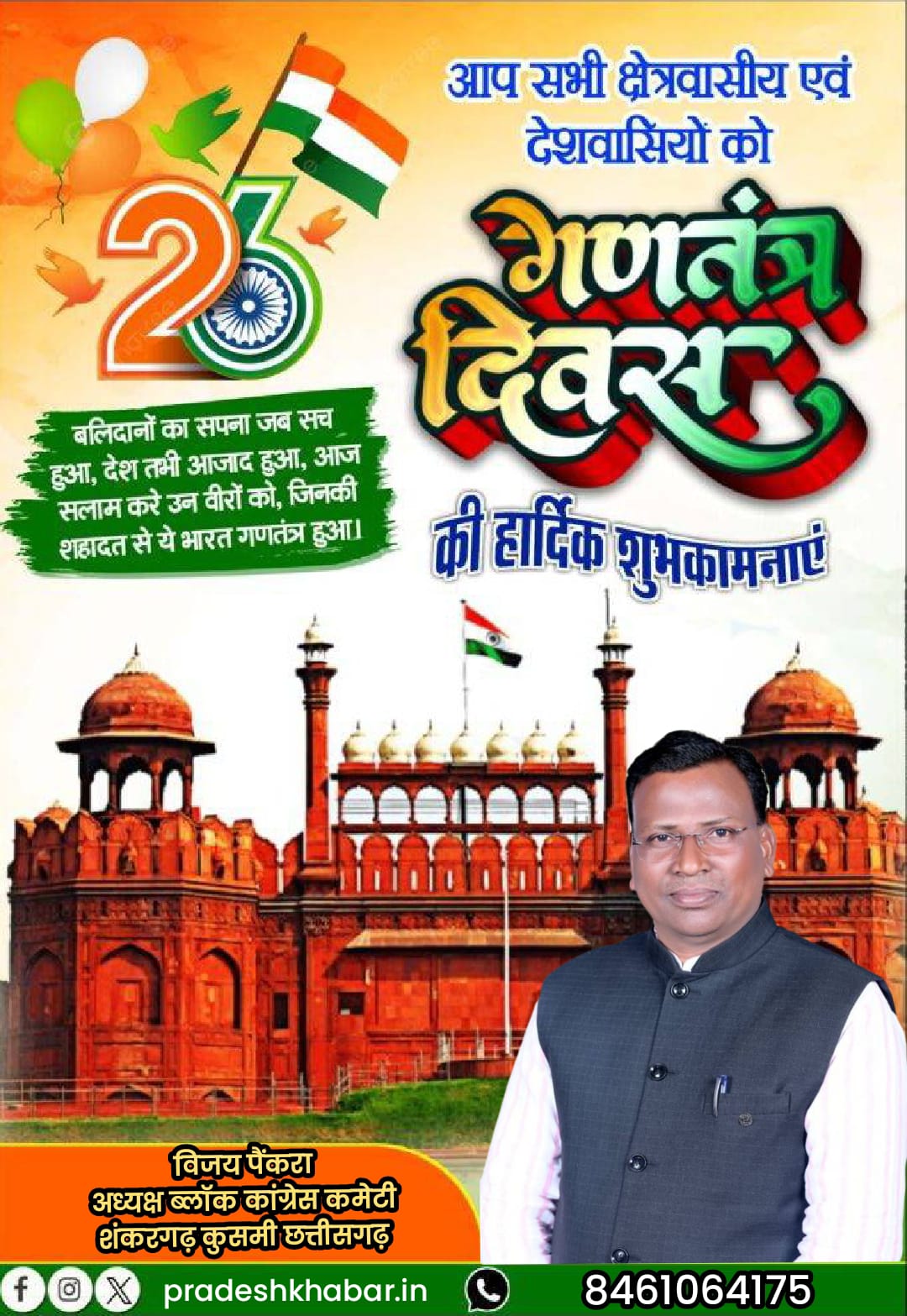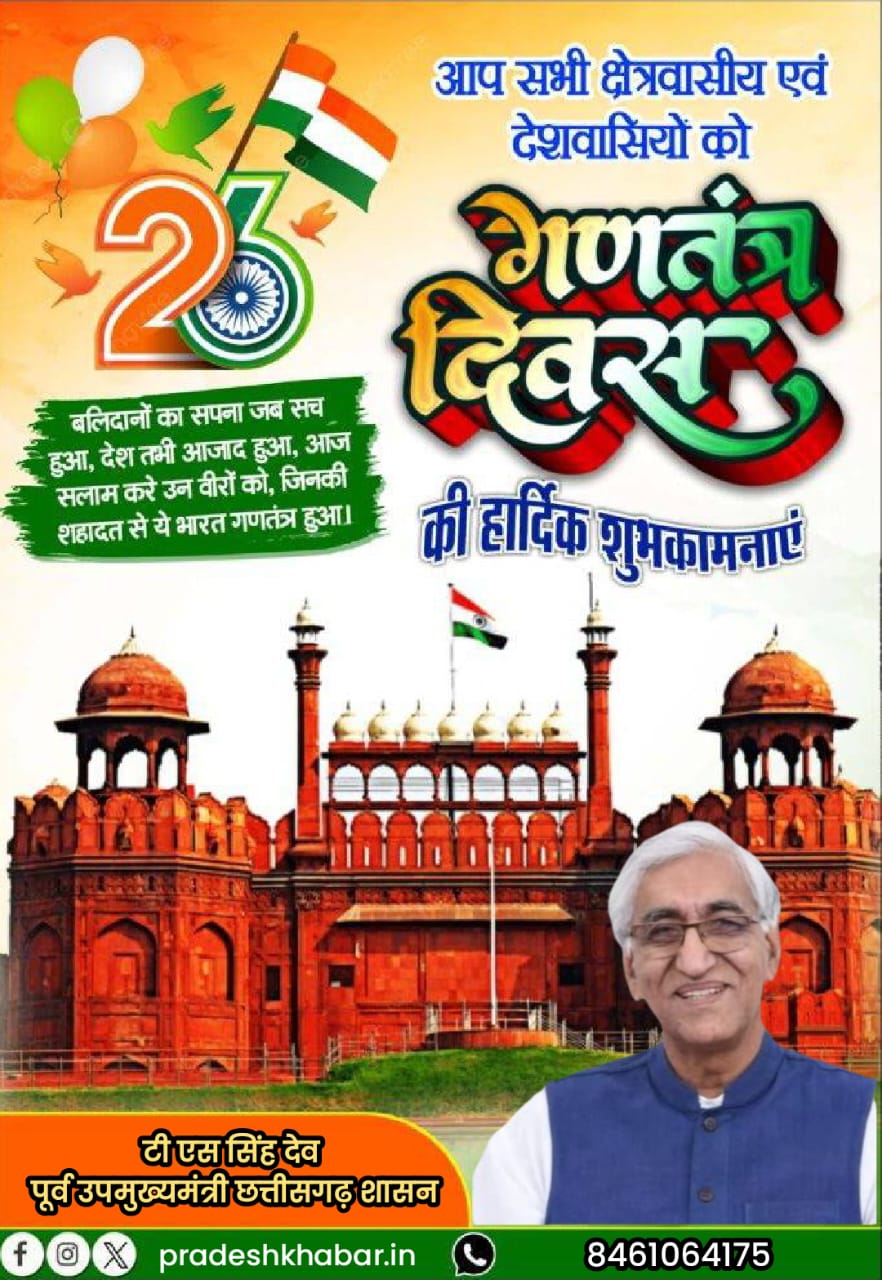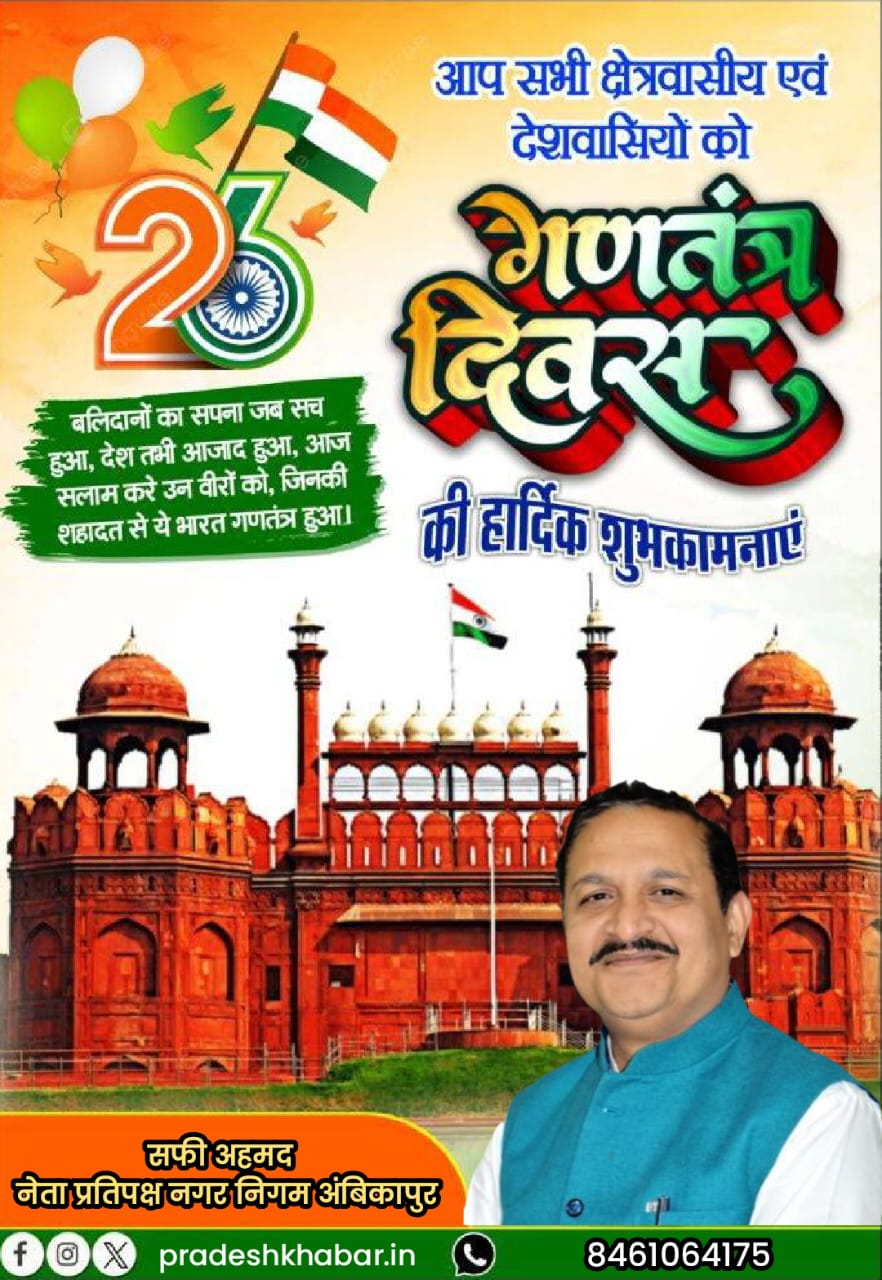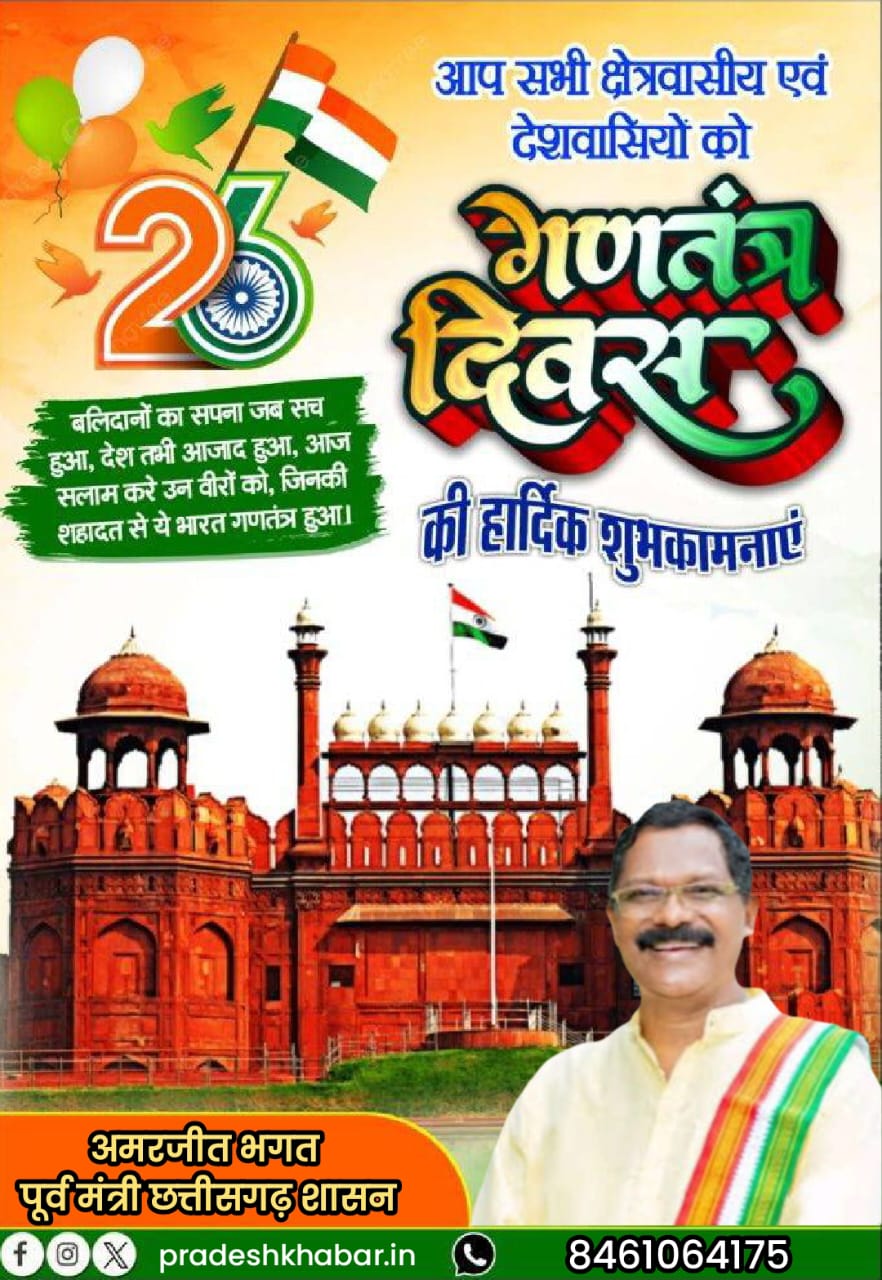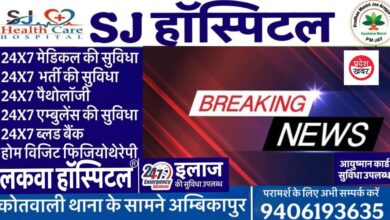भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा
भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा
हाइप्रिक्स एविएशन, जिसने भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित किया है, अब विस्तारित-दूरी के हमलों के लिए उन्नत रैमजेट आर्टिलरी शेल पर काम कर रहा है। इस विकास का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करना है।
भारत का निजी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र गति पकड़ रहा है, जिसमें घरेलू कंपनियाँ पारंपरिक रूप से सरकारी एजेंसियों और विदेशी रक्षा दिग्गजों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। एक उल्लेखनीय विकास बेंगलुरु स्थित हाइप्रिक्स एविएशन का है, जिसकी स्थापना देवमाल्या बिस्वास (23) और दिव्यांशु मंडोवारा (22) ने की है, जो लिक्विड-फ्यूल सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बन गई है – एक प्रणोदन तकनीक जो अगली पीढ़ी की मिसाइलों और उच्च गति वाले हवाई प्लेटफार्मों के लिए महत्वपूर्ण है।
हाइप्रिक्स ने हाल ही में अपने सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, तेज के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता हासिल की, जिसका जनवरी 2025 में आईआईटी मद्रास में राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र (एनसीसीआरडी) में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मैक 2 और मैक 4 के बीच की गति पर संचालन करने में सक्षम, तेज आयातित रक्षा प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के भारत के प्रयासों में एक मील का पत्थर है। रैमजेट इंजन, जो बिना यांत्रिक कंप्रेसर के दहन के लिए आने वाली हवा को संपीड़ित करके सुपरसोनिक गति बनाए रखते हैं, आधुनिक मिसाइल और उच्च गति वाले एयरोस्पेस सिस्टम का अभिन्न अंग हैं। तेज का विकास उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं का संकेत देता है, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले सरकारी अनुसंधान संस्थानों और विदेशी रक्षा ठेकेदारों तक ही सीमित था।
यह इंजन पारंपरिक रॉकेट-संचालित प्रणालियों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, जिसमें अधिक दक्षता, विस्तारित रेंज और निरंतर सुपरसोनिक गति शामिल है, जो इसे सुपरसोनिक मिसाइलों और उच्च गति वाले टोही प्लेटफार्मों के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाता है। प्रणोदन प्रणालियों में हाइप्रिक्स का काम रक्षा से परे है, कंपनी अगली पीढ़ी के एयरोस्पेस प्लेटफ़ॉर्म में अनुप्रयोगों की भी खोज कर रही है, जो दोनों क्षेत्रों में इसकी व्यापक तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है।
टेज़ के साथ अपनी सफलता के आधार पर, हाइप्रिक्स अब किरा एम1 विकसित कर रही है, जो एक ठोस ईंधन वाला रैमजेट-प्रोपेल्ड 155 मिमी विस्तारित-रेंज आर्टिलरी शेल है जिसे भारत की लंबी दूरी की आर्टिलरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तरल ईंधन वाले टेज़ के विपरीत, जो मिसाइलों और हवाई प्लेटफ़ॉर्म के लिए उपयुक्त है, किरा एम1 आर्टिलरी सिस्टम के लिए अनुकूलित ठोस ईंधन वाली रैमजेट तकनीक का उपयोग करता है। आर्टिलरी क्षमताएँ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख फ़ोकस हैं, क्योंकि सालाना 300,000 गोले का वर्तमान घरेलू उत्पादन 1.8 मिलियन गोले की अनुमानित युद्धकालीन आवश्यकता से काफी कम है। किरा एम1 जैसी तकनीकों में इस अंतर को भरने की क्षमता है, जो आयातित लंबी दूरी के आर्टिलरी गोले के लिए एक घरेलू, उच्च-प्रदर्शन विकल्प प्रदान करती है।
किरा एम1 में ठोस ईंधन से चलने वाला रैमजेट प्रणोदन शामिल है, जो इसे पारंपरिक 155 मिमी आर्टिलरी शेल की तुलना में लगभग चार गुना अधिक दूरी तक यात्रा करने में सक्षम बनाता है। सिस्टम को AI-निर्देशित नेविगेशन के साथ भी डिज़ाइन किया गया है, जो सटीकता को बढ़ाता है और संपार्श्विक क्षति को कम करता है – ऐसी विशेषताएँ जो आधुनिक युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस विकास ने पहले ही प्रमुख हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है, हाइप्रिक्स वर्तमान में सिस्टम के निहित विकास के लिए सेना डिज़ाइन ब्यूरो और आर्टिलरी निदेशालय के साथ चर्चा कर रहा है। ये जुड़ाव निजी क्षेत्र के नवाचार और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण प्रयासों के बीच बढ़ते संरेखण को उजागर करते हैं।
वैश्विक स्तर पर, रैमजेट-प्रोपेल्ड आर्टिलरी शेल के बाज़ार पर कुछ खिलाड़ियों का दबदबा है, जिसमें नैमो और बोइंग जैसी रक्षा दिग्गज कंपनियाँ इसी तरह की तकनीकों को आगे बढ़ा रही हैं। हालाँकि, हाइप्रिक्स का काम इस उन्नत आर्टिलरी सेगमेंट में भारत के निजी क्षेत्र के पहले प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे-जैसे सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री की वैश्विक मांग बढ़ती है, ऐसे विकास भारत को न केवल एक आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादक के रूप में बल्कि उन्नत सैन्य तकनीक के भविष्य के निर्यातक के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं।
रक्षा प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार भारत की रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति के भीतर एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2029 तक घरेलू रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ, सरकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रही है जहाँ घरेलू उद्यम रणनीतिक तकनीकी क्षमताओं में योगदान दे सकते हैं। तेज और किरा एम1 जैसी उन्नत प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम घरेलू खिलाड़ियों का उदय भारत के हथियार आयातक से उन्नत रक्षा और एयरोस्पेस प्रणालियों के संभावित वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में परिवर्तन को रेखांकित करता है।
उन्नत तोपखाना गोले, मिसाइल प्रणाली और सुपरसोनिक हवाई प्लेटफार्मों के बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो सैन्य व्यय में वृद्धि और युद्ध की बदलती आवश्यकताओं के कारण है। जैसे-जैसे निजी क्षेत्र के अधिक खिलाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर भारत की स्थिति मजबूत होगी, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी और अभिनव समाधान प्रदान करेगी।
भारत का रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ तकनीकी क्षमता और नीति समर्थन वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अभिसरण कर रहे हैं। हाइप्रिक्स जैसी कंपनियों की प्रगति आयात पर निर्भरता से स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार के उद्भव की ओर बदलाव का संकेत देती है, जिसमें रक्षा और एयरोस्पेस दोनों क्षेत्रों को अत्याधुनिक प्रणालियों की आपूर्ति करने की क्षमता है। आने वाले वर्ष यह निर्धारित करेंगे कि भारत का निजी रक्षा क्षेत्र इन तकनीकी प्रगति का कितना प्रभावी ढंग से स्केलेबल उत्पादन और दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में लाभ उठा सकता है।